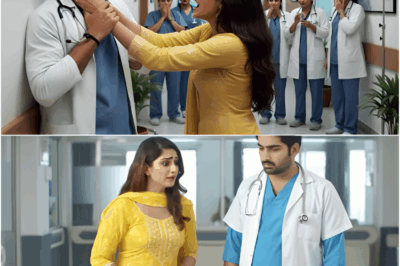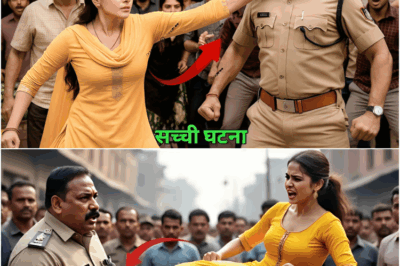जब बैंक के मालिक बैंक में बुजुर्ग बनकर गए मैनेजर ने धक्के मारकर निकला फिर जो हुआ.
.
.
एक बार की बात है, एक छोटे से गाँव में एक साधारण सा आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। रामू एक किसान था और अपनी फसल से ही अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।
गाँव में हर साल एक मेला लगता था, जो सभी गांववालों के लिए एक उत्सव की तरह होता था। इस मेले में लोग अपने-अपने गाँव से आते थे, खेल-खिलौनों का आनंद लेते थे, और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखते थे। रामू और सीता का सपना था कि इस बार वे अपने बच्चों को मेले में ले जाएंगे और उन्हें वहाँ की खुशियों का अनुभव कराएंगे।
मेले का दिन आया। रामू ने अपनी फसल से कुछ पैसे बचाए थे, जिससे उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। सीता ने घर में कुछ मिठाइयाँ बनाई थीं, जिन्हें वे मेले में ले जाने वाले थे। बच्चों का उत्साह देखने लायक था। वे बार-बार अपनी माँ से पूछते रहे कि क्या वे जल्दी चल सकते हैं।

जब वे मेले में पहुंचे, तो वहाँ का नजारा अद्भुत था। चारों ओर रंग-बिरंगे झूले, खेल-तमाशे, और खाने-पीने की stalls थीं। बच्चे झूले की तरफ दौड़ पड़े और रामू और सीता ने उन्हें वहाँ से दूर खड़े होकर देखा।
रामू ने सोचा, “यहाँ आकर बच्चों की खुशी देखना ही सबसे बड़ा सुख है।” उन्होंने सीता से कहा, “देखो, हमारे बच्चों की खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।” सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, “हाँ, और हम उनके लिए यह सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं।”
बच्चों ने झूले पर बैठकर खूब मजा किया। रामू और सीता ने भी मेले में घूमते हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन चखे। उन्होंने गाँव के अन्य लोगों से भी मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया।
लेकिन तभी अचानक एक घटना घटी। मेले में एक बड़ा हंगामा मच गया। एक आदमी चिल्ला रहा था, “चोर! मेरी जेब में से पैसे चोरी हो गए!” वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रामू ने देखा कि एक युवक, जो बहुत ही संदिग्ध लग रहा था, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था।
रामू ने उस युवक का पीछा किया। वह जानता था कि अगर वह उस युवक को पकड़ लेता है, तो शायद गाँव का नाम भी रोशन हो जाएगा। उसने दौड़ते हुए युवक को पकड़ लिया और shouted, “रुको! तुमने चोरी की है!”
युवक ने रामू को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे पकड़ लिया। वहाँ भीड़ में से कुछ लोग भी मदद के लिए आए और युवक को पकड़ लिया।
जब पुलिस आई, तो उन्होंने युवक को गिरफ्तार कर लिया। रामू ने पुलिस को बताया कि उसने कैसे युवक को पकड़ा। पुलिस ने रामू की तारीफ की और कहा, “आपने बहुत बहादुरी से काम किया है।”
इस घटना के बाद, रामू गाँव का हीरो बन गया। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। उसने अपने बच्चों को बताया कि सच्ची बहादुरी क्या होती है और कैसे हमें हमेशा सही के लिए खड़ा रहना चाहिए।
मेले का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। लोग रामू की बहादुरी की चर्चा कर रहे थे और उसने अपने बच्चों को सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।
इस घटना ने रामू के जीवन को बदल दिया। गाँव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे और उसके परिवार की स्थिति भी बेहतर हो गई। रामू ने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और उन्हें यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है।
इस तरह, रामू की कहानी गाँव में एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी और ईमानदारी से जीवन में कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।
समय बीतता गया, और रामू के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। गाँव में एक नई पीढ़ी आई, जो रामू के आदर्शों को अपनाने लगी।

रामू ने अपने बच्चों को बताया कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें हमेशा धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है।
गाँव में एक नई शुरुआत हुई। लोग अब एक-दूसरे की मदद करने लगे और गाँव का माहौल खुशहाल हो गया। रामू की कहानी अब गाँव की पहचान बन गई थी।
इस तरह, रामू ने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गाँव को एक नया रास्ता दिखाया। उसकी बहादुरी और ईमानदारी ने सभी को एकजुट किया और गाँव को एक नई दिशा दी।
समाप्त!
.
.
लावारिस मरीज़ की सेवा करती थी नर्स, 1 महीने बाद जब मरीज़ का अरबपति बेटा आया तो अस्पताल में जो हुआ
दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। यहाँ की हवा में दवाओं की गंध, मरीज़ों के कराहने की आवाज़ें और डॉक्टरों-नर्सों की भागदौड़ घुली रहती थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ हर रोज़ ज़िंदगी और मौत के बीच जंग चलती थी।
इसी जंग की एक सिपाही थी कविता। 28 साल की कविता पिछले पाँच सालों से इस अस्पताल के जनरल वार्ड में नर्स का काम कर रही थी। वह एक छोटे से गाँव से आई थी और उसके सपने भी छोटे थे—बस अपने बूढ़े माँ-बाप की देखभाल करना और छोटे भाई की पढ़ाई पूरी करवाना।
कविता के लिए उसकी ड्यूटी सिर्फ़ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन थी। जहाँ दूसरी नर्सें काम को बोझ समझकर निपटाती थीं, वहीं कविता हर मरीज़ की तकलीफ़ को अपना समझकर उसकी सेवा करती थी। उसके स्वभाव की इसी नरमी और दयालुता के कारण मरीज़ उसे दीदी कहकर पुकारते थे।
बेड नंबर 24: लावारिस बाबा
अस्पताल का सिस्टम और कुछ कर्मचारियों का कठोर व्यवहार अक्सर कविता के दिल को दुखाता था, ख़ासकर तब जब कोई लावारिस मरीज़ आता था। लावारिस मरीज़ यानी एक ऐसा इंसान जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता—न कोई नाम, न कोई पता, न कोई रिश्तेदार।
एक महीने पहले ऐसा ही एक मरीज़ आया था। पुलिस को वह एक पार्क की बेंच पर बेहोशी की हालत में मिला था—एक बूढ़ा आदमी, कोई 70 साल का। डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है और वह गहरे कोमा में है। उसके बचने की उम्मीद न के बराबर थी।
उसे लावारिस मानकर वार्ड के सबसे आख़िरी बिस्तर, बेड नंबर 24 पर डाल दिया गया।
सबके लिए वह सिर्फ़ बेड नंबर 24 था, पर कविता के लिए वह एक बेबस, लाचार इंसान था। उसे उस बूढ़े आदमी के झुर्रियों भरे चेहरे में अपने गाँव में रहते पिता की झलक दिखाई दी। उस दिन से कविता ने उस लावारिस मरीज़ की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठा ली।
बेटी की तरह सेवा
उसका नाम किसी को नहीं पता था, तो कविता ने मन ही मन उसे ‘बाबा’ कहना शुरू कर दिया। वह अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी घंटों बाबा के पास बैठी रहती। वह रोज़ उनके शरीर को स्पंज करती, उनके कपड़े बदलती और समय पर उनकी नली से जाने वाली खुराक का ध्यान रखती।
जब दूसरे कर्मचारी कहते, “क्यों अपना वक़्त बर्बाद कर रही हो कविता, इसका कोई नहीं है, दो-चार दिन का मेहमान है, चला जाएगा,” तो कविता मुस्कुरा कर कहती, “कोई नहीं है तभी तो हम हैं। नर्स का फ़र्ज़ सिर्फ़ दवा देना नहीं, सेवा करना भी होता है।”
वह अक्सर बाबा से बातें करती, भले ही वे कोमा में थे। वह उन्हें अपने गाँव के क़िस्से सुनाती और कभी-कभी भगवत गीता के श्लोक भी पढ़कर सुनाती। उसने अपनी छोटी सी तनख़्वाह से पैसे बचाकर बाबा के लिए एक नया कंबल और कुछ साफ़ कपड़े भी ख़रीदे थे।
पूरा एक महीना गुज़र गया। बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं था, पर कविता ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी।
चमत्कार और पहचान
और फिर एक दिन वह हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
उस दिन सुबह अस्पताल के बाहर एक काले रंग की चमचमाती बेंटले कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरा नौजवान था राजीव मेहरा—लंदन का एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन। वह भागता हुआ रिसेप्शन पर पहुँचा। उसने अपने फ़ोन से एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा, “क्या यह आदमी यहाँ भर्ती है? इनका नाम रामनाथ मेहरा है।”
रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में नाम ढूँढ़ने लगी, “नहीं सर, इस नाम का कोई मरीज़ यहाँ नहीं है।”
राजीव का दिल बैठ गया। वह पिछले एक महीने से अपने पिता को पागलों की तरह ढूँढ़ रहा था। रामनाथ मेहरा, उसके पिता, एक स्वाभिमानी इंसान थे। बिज़नेस को लेकर बाप-बेटे में अनबन हुई थी, पर राजीव अपने पिता से बहुत प्यार करता था।
वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी एक वार्ड बॉय ने तस्वीर देखकर कहा, “अरे साहब, यह चेहरा तो जाना-पहचाना लग रहा है। यह तो अपने वार्ड के बेड नंबर 24 वाले लावारिस बाबा हैं।”
“लावारिस?” राजीव के कानों में यह शब्द ज़हर की तरह लगा। मेरे पिता और लावारिस?
वह बेचैनी में वार्ड बॉय के पीछे-पीछे भागा। जब वह वार्ड के अंदर पहुँचा, तो उसने देखा कि आख़िरी बिस्तर पर उसके पिता लेटे हुए थे, मशीनों से घिरे हुए।
वह गुस्से में डॉक्टरों पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक नर्स पर पड़ी जो बड़े प्यार और अपनेपन से उसके पिता का चेहरा एक गीले कपड़े से पोंछ रही थी। वह उनसे धीरे-धीरे बातें भी कर रही थी। “बाबा, आज आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। जल्दी से आँखें खोल दीजिए न।”
यह कविता थी, जो अपने काम में मग्न थी।
एहसान और निस्वार्थता
तभी वही वार्ड बॉय राजीव के पास आकर धीरे से बोला, “साहब, अगर आज आपके पिताजी ज़िंदा हैं, तो सिर्फ़ इस कविता दीदी की वजह से। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब भी इन्होंने अकेले, एक सगी बेटी की तरह, इनकी सेवा की है।”
राजीव की आँखें भर आईं। वह धीरे-धीरे चलकर कविता के पास पहुँचा।
“मेरा नाम राजीव मेहरा है। और यह लावारिस मरीज़ जिन्हें आप बाबा कहती हैं, यह मेरे पिता हैं—श्री रामनाथ मेहरा।”
कविता की आँखें आश्चर्य से फैल गईं। उसकी आवाज़ में शिकायत और गुस्सा था, “आपके… आपके पिता? तो आप इतने दिनों से कहाँ थे?”
राजीव ने नज़रें झुका लीं। “मैं जानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी ग़लती हुई है। पर मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊँ? आपने मेरे पिता के लिए जो किया…”
कविता ने उसे बीच में ही रोक दिया। “एहसान कैसा साहब? यह तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की।”
राजीव को लगा जैसे इस साधारण सी नर्स के सामने उसका अरबों का साम्राज्य, उसकी सारी दौलत सब कुछ बौना पड़ गया हो।
उसने फ़ौरन अपने फ़ोन से देश के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में बात की और एक एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने को कहा। फिर वह कविता की ओर मुड़ा और चेक बुक से एक बड़ी रक़म का चेक काटकर उसे देने लगा।
कविता ने हाथ पीछे कर लिए। “माफ़ कीजिएगा साहब। मैं यह नहीं ले सकती। मैंने जो भी सेवा की, वह पैसों के लिए नहीं की थी।”
राजीव ने ज़ोर दिया, “पर मैं अपने मन की शांति के लिए यह करना चाहता हूँ।”
कविता ने दृढ़ता से कहा, “अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो बस यह दुआ कीजिएगा कि बाबा जल्दी ठीक हो जाएँ। मेरे लिए उससे बड़ा कोई इनाम नहीं होगा।”
दौलत से बड़ा इनाम
राजीव कविता की इस निस्वार्थता के आगे नतमस्तक हो गया। उसने कुछ सोचा और फिर एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया।
उसने अस्पताल के डीन को अपने पास बुलाया। “डीन साहब, मैं अपने पिता श्री रामनाथ मेहरा के नाम पर इस शहर में एक सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। जहाँ हर ग़रीब और लावारिस मरीज़ का मुफ़्त में इलाज होगा। और मैं चाहता हूँ कि उस अस्पताल की मुख्य ट्रस्टी और हेड एडमिनिस्ट्रेटर कविता जी हों।”
यह सुनकर कविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। “मैं? साहब, मैं तो एक मामूली नर्स हूँ। मुझसे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे सँभलेगी?”
राजीव मुस्कुराया। “कविता जी, जो इंसान बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी उम्मीद के, किसी की इतनी सेवा कर सकता है, उससे बड़ी ज़िम्मेदारी दुनिया में कोई नहीं सँभाल सकता। आपकी इंसानियत ही आपकी सबसे बड़ी क़ाबिलियत है। और हाँ, आपकी आगे की पढ़ाई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स, सब विदेश में होगा। इसका सारा ख़र्चा मेहरा फाउंडेशन उठाएगा।”
कविता के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी आँखों से बस आँसू बह रहे थे।
उपसंहार
कुछ महीनों बाद रामनाथ मेहरा जी बिल्कुल ठीक हो गए। बाप-बेटे के बीच की दूरियाँ भी मिट गईं। उन्होंने कविता को अपनी बेटी की तरह अपना लिया।
और कुछ सालों बाद, शहर के बीचों-बीच एक शानदार रामनाथ मेहरा चैरिटेबल हॉस्पिटल खड़ा था जिसकी डायरेक्टर थी कविता। वह आज भी उतनी ही नरमी और दयालुता से मरीज़ों की सेवा करती थी, पर अब उसके पास हज़ारों बाबा और अम्मा की ज़िम्मेदारियाँ थीं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाला आपकी नेकी को देख रहा होता है, और वह सही समय पर सही तरीक़े से उसका फल ज़रूर देता है।
न्याय की आवाज़: एक भीखारिन का सच
सन्नाटा और एक साया
जयपुर शहर के व्यस्त कोर्ट परिसर में रोज़ की तरह गहमागहमी थी, मगर कोर्ट रूम संख्या तीन में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सबकी निगाहें एक-दूसरे पर टिके हुए थीं। यह शहर के सबसे चर्चित निर्माण घोटाले की सुनवाई थी, जिसमें कई बड़े रसूखदार लोग फँसे थे।
तभी, कोर्ट रूम का दरवाज़ा खुला और अंदर दाख़िल हुई एक बूढ़ी औरत—एक फटे हाल भीखारिन। लोगों की निगाहें तिरस्कार और आश्चर्य से भर गईं। उनकी साड़ी फटी थी, आँखें थकी हुई थीं और उनके काँपते पैरों के साथ गरीबी का एक बोझिल साया अंदर आ गया।
मगर अगले ही पल, जो हुआ, उसने सबको स्तब्ध कर दिया।
न्यायाधीश जस्टिस राजेश अग्रवाल, जो अपने सख्त और निष्पक्ष फैसलों के लिए मशहूर थे, अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी मेज़ की ओर इशारा किया और एक सम्मान भरी आवाज़ में कहा, “आइए, आप यहाँ बैठिए।”
पूरा कोर्ट सकते में था। आख़िर क्यों? क्यों एक भीखारिन के लिए एक न्यायाधीश ने अपनी कुर्सी छोड़ दी? यह सवाल हवा में गूँज रहा था।
अम्मा: कोर्ट के बाहर का सन्नाटा
कोर्ट के बाहर, एक बूढ़ी भीखारिन महिला हर दिन चुपचाप बैठी रहती थी। लोग उसे ‘अम्मा’ कहते थे, तो कुछ हिकारत से पागल कहकर आगे बढ़ जाते। वह कुछ नहीं बोलती थी। उनके सामने रखा टिन का कटोरा अक्सर खाली रहता, मगर उनकी आँखों में कुछ था—जैसे वह किसी को पहचानती हो, कुछ कहना चाहती हो।
हर सुबह ठीक चार बजे, अम्मा कोर्ट परिसर के पास बने शारदा मंदिर के पास आकर बैठ जातीं। उनकी कमर झुकी हुई थी, फिर भी वह पूरी शान से सीधी बैठतीं, जैसे कोई पुराना सैनिक अपनी आख़िरी सलामी दे रहा हो। उनकी नज़रें सड़क पर टिकी रहतीं, मगर अक्सर कोर्ट के गेट पर ठहर जाती थीं। वह कोर्ट को देखती थीं, पर कभी कुछ माँगती नहीं थीं।
न्यायाधीश का अजीब आदेश
उस दिन, 11 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। तीखी बहस और वकीलों की दलीलों के बीच एक तनाव भरा माहौल था। तभी, जस्टिस राजेश अग्रवाल की नज़र खिड़की से बाहर चली गई। उनकी आँखों में कोई पुरानी याद कौंध गई।
उन्होंने अपने क्लर्क की तरफ़ देखा और धीरे से कहा, “क्या कोर्ट परिसर के मंदिर के बाहर जो बूढ़ी भीखारिन बैठी है, उसे तुरंत अंदर बुलाया जा सकता है?”
कोर्ट रूम में अजीबोगरीब फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक भीखारिन को कोर्ट में बुलाने की क्या ज़रूरत थी?
दो सुरक्षाकर्मी अम्मा के पास पहुँचे। अम्मा ने धीरे से सिर उठाया, अपनी छड़ी उठाई और काँपते हुए खड़ी हुईं। वह बिना सवाल किए, बिना कुछ बोले, कोर्ट रूम की ओर चल पड़ीं।
अंदर दाख़िल होने पर, न्यायाधीश ने उन्हें बैठने के लिए कहा। अम्मा काँपते हुए बेंच पर बैठीं। उनके चेहरे पर न डर था, न गर्व, बस एक गहरी शांति।
न्यायाधीश ने पूछा, “आप रोज़ यहाँ आती हैं। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं?”
अम्मा की आवाज़ में हल्का कंपन था, मगर शब्दों में एक गहरी ताक़त: “कहना तो बहुत कुछ था, मगर सुनने वाला कोई नहीं था… इसलिए चुप हो गई।”
“आप रोज़ इस कोर्ट को देखती हैं। कोई ख़ास वजह?” न्यायाधीश ने पूछा।
अम्मा ने एक पल के लिए आँखें बंद कीं और फिर बोलीं, “यह वही जगह है, जहाँ मैंने कभी न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी। जहाँ मैं कभी अधिवक्ता हुआ करती थी।“
रमा देवी का त्याग
यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। एक भीखारिन जो सड़क किनारे बैठी रहती थी, वह अधिवक्ता थी?
अम्मा ने अपने पुराने झोले से एक पीला, फटा हुआ लिफ़ाफ़ा निकाला। उसमें कुछ पुराने कागज़ थे—एक वकालतनामा, एक पुराना अधिवक्ता पहचान पत्र और एक अधूरी याचिका। जस्टिस अग्रवाल जैसे-जैसे उन कागज़ों को पढ़ते गए, उनके माथे की लकीरें गहरी होती गईं।
“आप अधिवक्ता थीं?”
“हाँ,” अम्मा ने जवाब दिया, “मगर बेटी की ग़लती का इल्ज़ाम मुझ पर आया। मैं चुप रही, सोचा बेटी बच जाए। अदालत ने मुझे दोषी ठहराया। मेरी सारी संपत्ति ज़ब्त हो गई। जब जेल से बाहर आई, तो बेटी सब कुछ बेचकर शहर छोड़ चुकी थी।”
कोर्ट में मौजूद हर शख़्स की आँखें नम थीं। जो अधिवक्ता पहले अम्मा का मज़ाक़ उड़ाते थे, वह अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे।
जस्टिस राजेश अग्रवाल ने अम्मा का हाथ थाम लिया। उन्होंने भरे गले से कहा, “हमने न्याय को सिर्फ़ क़ानून की किताबों में बाँध दिया, मगर आपने इसे अपनी ज़िंदगी में जिया।”
गुरु और शिष्य
अगले दिन, जयपुर के अख़बारों में एक ही हेडलाइन थी: “भीखारिन नहीं, पूर्व अधिवक्ता: न्यायाधीश ने छोड़ा अपनी कुर्सी, किया स्वागत।”
असल में, अम्मा का नाम श्रीमती रमा देवी था। वह एक समय में जयपुर के कोर्ट में सबसे सम्मानित नाम थीं। वह गरीबों के मुक़दमे मुफ़्त में लड़तीं, कभी घूस नहीं लेती थीं। मगर उनकी अपनी बेटी, प्रीति, ने उन्हें धोखा दिया। प्रीति एक निर्माण घोटाले में फँस गई थी और उसने अपनी ख़राब क्रेडिट हिस्ट्री के कारण सारी संपत्ति और दस्तावेज़ माँ के नाम पर कर दिए थे।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जस्टिस अग्रवाल ने अम्मा से पूछा था, “आपने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ कुछ क्यों नहीं कहा?”
अम्मा ने सिर झुका कर जवाब दिया, “मैंने ज़िंदगी भर क़ानून के लिए लड़ा, मगर जब मेरी बेटी सामने आई, तो माँ हार गई।”
उस दिन मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती आरती वर्मा ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, “माई लॉर्ड, यह मुक़दमा सिर्फ़ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, यह सिस्टम की चूक की मिसाल है। मैं याचिका दायर करती हूँ कि इस मामले की दोबारा सुनवाई हो।”
न्यायाधीश ने सहमति में सिर हिलाया।
सत्य की जीत
जस्टिस राजेश अग्रवाल कोई साधारण न्यायाधीश नहीं थे। 20 साल पहले अजमेर यूनिवर्सिटी में रमा देवी उनकी प्रेरणा थीं। उनकी एक बात आज भी राजेश की डायरी में लिखी थी: “अगर वकालत को सिर्फ़ धंधा समझोगी, तो यह दुकान बन जाएगी। मगर अगर इसे इंसान की आवाज़ समझोगी, तो यह इबादत बन जाएगी।” राजेश भावुक थे। उन्होंने कहा, “मैं यह मुक़दमा व्यक्तिगत रूप से सुनूँगा।”
आखिरकार, उनकी बेटी प्रीति को कोर्ट में पेश किया गया। महँगी गाड़ी, ब्रांडेड सूट… मगर आँखें झुकी हुईं। जब न्यायाधीश ने पूछा, “संपत्ति अपने माँ के नाम क्यों ली?” तो उसने कबूल किया, “मेरी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब थी। मैंने उनके दस्तख़त नकली किए।”
पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अम्मा चुप रहीं, उन्होंने बस आँखें बंद कर लीं।
न्यायाधीश ने अपना फ़ैसला सुनाया:
श्रीमती रमा देवी निर्दोष हैं।
उन्हें तुरंत दोबारा वकालत का लाइसेंस दिया जाए।
उन्हें ₹25 लाख की मानहानि राशि दी जाए।
सरकार सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगे।अगले दिन अम्मा फिर कोर्ट के बाहर बैठी थीं, मगर अब लोग उनके सामने झुक रहे थे। कोई उनके पैर छू रहा था, कोई उन्हें सम्मान दे रहा था।
न्यायाधीश राजेश अग्रवाल चुपके से उनके पास आए और बैठ गए। “आज मैंने न्याय नहीं किया,” उन्होंने कहा, “आज मैंने सिर्फ़ एक क़र्ज़ चुकाया है।”
अम्मा मुस्कुराईं। “बेटी, आज तू सिर्फ़ न्यायाधीश नहीं, इंसान भी बनी है।”
यह कहानी सिर्फ़ रमा देवी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने सच के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी। जयपुर के कोर्ट के बाहर अम्मा की कहानी आज भी गूँजती है—कि विश्वास, न्याय और हौसला सालों की तकलीफ़ों के बाद भी नहीं टूटता।
यह कहानी प्रेरणा और भावनाओं से भरी है। क्या आप रमा देवी के पुनर्जीवित हुए वकालत के करियर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, या जस्टिस अग्रवाल की प्रतिक्रिया पर?
कचरा उठाने वाली लड़की को कचरे में मिले किसी के घर के कागज़ात, लौटाने गई तो जो हुआ वो आप सोच भी नही
“ईमानदारी की किरण: आशा की कहानी”
दिल्ली, भारत का दिल। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। जहां एक तरफ चमचमाती इमारतें, आलीशान कोठियां हैं, वहीं दूसरी ओर झुग्गी बस्तियों में लाखों जिंदगियां हर रोज बस एक और दिन जीने के लिए संघर्ष करती हैं। ऐसी ही एक बस्ती जीवन नगर में, टीन की छत और त्रिपाल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी 17 साल की आशा किरण अपनी मां शांति के साथ। उनका घर बेहद साधारण था – एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, दूसरे में पुरानी चारपाई, और बारिश में टपकती छत, जो उनके सपनों में भी खलल डाल देती थी।
आशा के पिता सूरज एक ईमानदार मजदूर थे, जिनका सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अफसर बने और बस्ती में रोशनी लाए। लेकिन तीन साल पहले एक हादसे में सूरज का देहांत हो गया। मां शांति बीमारी और ग़म के बोझ से टूट गईं। अब घर की सारी जिम्मेदारी आशा के कंधों पर आ गई थी। उसे आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब उसकी दुनिया थी – एक बड़ा सा बोरा, जिसे वह हर सुबह पीठ पर लादकर कचरा बीनने निकल पड़ती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जो भी पैसे मिलते, उसी से घर चलता और मां की दवाइयां आतीं।
आशा के हाथ सख्त हो चुके थे, मगर दिल बहुत नरम था। पिता का सपना उसकी आंखों में अब भी जिंदा था। वह हर रात अपनी पुरानी किताबें पढ़ती थी, लेकिन हालात ने उसके हाथों में किताब की जगह कचरे का बोरा थमा दिया था।
एक दिन, आशा वसंत विहार की गलियों में कचरा बीन रही थी। एक सफेद कोठी के बाहर उसे एक मोटी लेदर की फाइल मिली। वह फाइल आमतौर पर कचरे में नहीं फेंकी जाती। आशा ने सोचा, शायद इसमें कुछ रद्दी कागजात होंगे। दिन के अंत में जब वह अपनी झोपड़ी लौटी, तो मां की खांसी सुनकर उसका दिल बैठ गया। रात में, जब मां सो गई, तो आशा ने वह फाइल खोली। उसमें सरकारी मोहर लगे कई कागजात थे। आशा को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी, मगर उसने नाम पढ़ा – सुरेश आनंद। और एक शब्द – प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। उसे समझ आ गया कि ये किसी की जमीन के असली कागजात हैं।
एक पल को उसके मन में आया कि इन कागजातों से उसकी गरीबी मिट सकती है। मगर तुरंत उसे पिता की बात याद आई – “बेईमानी की रोटी खाने से अच्छा है, ईमानदारी का भूखा सो जाना।” आशा ने तय किया कि वह कागजात लौटाएगी।
अगली सुबह, आशा काम पर नहीं गई। उसने अपनी सबसे साफ सलवार कमीज पहनी, कागजात को प्लास्टिक की थैली में रखा और मां से कहकर वसंत विहार पहुंच गई। वहां हर गेट पर गार्ड से आनंद विला का पता पूछती रही, मगर किसी ने मदद नहीं की। तीन दिन तक यही सिलसिला चला। घर में खाने के लाले पड़ने लगे, मां भी चिंता करने लगी। मगर आशा ने हार नहीं मानी।
पांचवे दिन, जब आशा लगभग टूट चुकी थी, एक डाकिया आया। उसने कागज देखकर बताया कि सुरेश आनंद की कोठी वसंत कुंज में है, न कि वसंत विहार में। आशा तुरंत वहां पहुंची। आनंद विला के गेट पर उसने सुरेश आनंद से मिलने की बात कही। सुरेश आनंद की पत्नी सविता जी ने शक के बावजूद उसे अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में सुरेश आनंद आए। आशा ने कांपते हाथों से फाइल दी। कागजों को देखते ही सुरेश आनंद की आंखों में आंसू आ गए। ये वही कागजात थे, जिनके बिना उनका करोड़ों का केस हारने वाले थे।
आशा ने पूरी कहानी सच-सच बता दी। सुरेश आनंद ने नोटों की गड्डी निकालकर आशा को एक लाख रुपये देने चाहे। मगर आशा ने सिर झुका लिया, “मेरे पिता कहते थे नेकी का सौदा नहीं किया जाता। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है।”
सुरेश आनंद आशा की ईमानदारी से भीतर तक हिल गए। उन्होंने पूछा, “तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम अफसर बनो?” आशा ने सिर हिलाया। सुरेश आनंद ने तय किया कि आशा की पढ़ाई का सारा खर्च आनंद फाउंडेशन उठाएगा। उसकी मां का इलाज शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में होगा। इसके अलावा, उन्होंने आशा को एक बंद पड़ी किराने की दुकान और उसके ऊपर का फ्लैट दे दिया, ताकि वह मेहनत से अपना घर चला सके।
आशा की जिंदगी बदल गई। उसकी मां स्वस्थ हो गईं, वे नए घर में शिफ्ट हो गईं। आशा ने पढ़ाई फिर से शुरू की, स्कूल और फिर कॉलेज गई। दुकान अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई, सिर्फ सामान के लिए नहीं, बल्कि आशा की ईमानदारी और मीठे स्वभाव के लिए। सुरेश आनंद और उनका परिवार अब आशा के लिए एक परिवार की तरह हो गए।
कई साल बाद, आशा ने ग्रेजुएशन पूरी की, अफसर बनी, मगर अपनी दुकान बंद नहीं की। उसने वहां और जरूरतमंद लड़कियों को काम पर रखा, ताकि वे भी इज्जत से जिंदगी जी सकें। वह अक्सर अपनी मां से कहती, “मां, बाबूजी ठीक कहते थे, ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, मगर उसकी मंजिल बहुत सुंदर होती है।”
कहानी से सीख:
यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, हमें अपनी अच्छाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेकी की रोशनी देर-सवेर हमारी जिंदगी के हर अंधेरे को मिटा ही देती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
ईमानदारी का संदेश हर दिल तक पहुंचे – यही आशा है!
.
.
15 साल की बेटी ने अपाहिज जज से कहा की मेरे पिता को छोड़ दें, मै आपको कुछ ऐसा बताउंगी कि आप चलने

सच्चाई की जीत: एक बेटी, एक जज और एक चमत्कार
दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट का खचाखच भरा कोर्ट रूम नंबर चार। वहां एक अधेड़ उम्र का साधारण सा आदमी कटघरे में खड़ा था—रवि शर्मा। एक सरकारी स्कूल का लाइब्रेरियन। उसकी पूरी जिंदगी ईमानदारी और किताबों के बीच बीती थी, लेकिन आज उस पर बैंक में करोड़ों के गबन का गंभीर आरोप था। सारे गवाह, सबूत, कागजात उसके खिलाफ थे। ऐसा लग रहा था कि उसका दोषी साबित होना बस वक्त की बात है।
न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे जस्टिस आनंद सिन्हा। कठोर, तेज दिमाग, ईमानदार और सख्त मिजाज। उनके लिए कानून सिर्फ तथ्यों और सबूतों का खेल था, भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भावनाओं के एक तूफान से गुजर चुकी थी। तीन साल पहले एक भयानक कार हादसे में वे कमर के नीचे से अपाहिज हो गए थे। उस हादसे ने उनके पैर ही नहीं, उनकी खुशियां भी छीन ली थीं। गाड़ी का ड्राइवर आज तक पकड़ा नहीं गया था। जस्टिस सिन्हा अब व्हीलचेयर पर थे—शारीरिक ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी अपंग
कोर्ट रूम के कोने में बैठी थी 15 साल की अनन्या—रवि शर्मा की बेटी। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी आग थी। उसे विश्वास था कि उसके पिता निर्दोष हैं। जब से पिता गिरफ्तार हुए, उसकी दुनिया बदल गई थी। स्कूल के दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार मुंह फेर चुके थे। वह स्कूल जाती, जेल में पिता से मिलती, घर आकर बीमार मां को संभालती। रात-रात भर केस की फाइलें पढ़ती, शायद कोई सुराग मिल जाए। वह जानती थी, जिस दिन बैंक में गबन हुआ, वह अपने पिता के साथ घर पर थी—लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं था।
मुकदमा अंतिम चरण में पहुंच चुका था। सरकारी वकील ने अंतिम दलीलें पेश कीं, सबको लग रहा था—रवि शर्मा को कम से कम 10 साल की सजा होगी। जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अनन्या के लिए वह रात कयामत थी। उसे पता था, कल सुबह उसके पिता उससे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। उसने एक आखिरी हताश कोशिश करने का फैसला किया—एक ऐसा कदम जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता।
अनन्या ने किसी तरह पिता के वकील से जस्टिस सिन्हा के घर का पता मालूम किया। शाम को जब जस्टिस सिन्हा का काफिला उनके बंगले पर पहुंचा, अनन्या पहले से वहां मौजूद थी। जैसे ही सहायक ने उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया, अनन्या दौड़कर सामने आ गई। सुरक्षा गार्डों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह शेरनी की तरह दहाड़ उठी—”मुझे जज साहब से मिलना है!” जस्टिस सिन्हा ने गुस्से से देखा, उन्हें लगा—यह लड़की सहानुभूति पाने के लिए नाटक कर रही है। “तुम्हें पता है, यह अदालत की अवमानना है?” उन्होंने कहा। लेकिन अनन्या की आंखों में डर नहीं था।
उसने कांपती आवाज को स्थिर करते हुए ऐतिहासिक वाक्य कहा—”जज साहब, मेरे पिता को छोड़ दीजिए। वह बेकसूर हैं। अगर आप उन्हें सजा नहीं देंगे, तो मैं वादा करती हूं—मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी कि आप फिर से चलने लगेंगे।” सन्नाटा छा गया। जस्टिस सिन्हा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा, यह लड़की उनके सबसे गहरे जख्म का मजाक उड़ा रही है। “तुम न्याय का सौदा करने आई हो? मेरे लिए न्याय किसी चमत्कार से ज्यादा कीमती है और मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। दफा हो जाओ, वरना गिरफ्तार करवा दूंगा!”
अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह हिली नहीं। “मैं सुबह कोर्ट में आपका इंतजार करूंगी,” बस इतना कहकर चली गई।
उस रात जस्टिस सिन्हा सो नहीं पाए। उसके शब्द—”आप फिर से चलने लगेंगे”—उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया था, सब ने कह दिया था—रीढ़ की चोट लाइलाज है। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन सालों बाद किसी ने उनके अंदर उम्मीद की चिंगारी छुआ दी थी। वे बेचैन थे, बार-बार एक्सीडेंट की रात याद कर रहे थे।
उधर, अनन्या घर में पिता के पुराने सामान को देख रही थी। तभी उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कॉलेज के दिनों की तस्वीरें और डायरियां थीं। एक तस्वीर देखकर वह चौंक गई—पिता के साथ खड़ा दोस्त कोई और नहीं, बल्कि गिरीश था। वही गिरीश, जो केस का मुख्य गवाह था और जिसकी गवाही ने ही उसके पिता को मुजरिम साबित किया था।
अनन्या ने कांपते हाथों से डायरी खोली। जैसे-जैसे पन्ने पलटे, सालों पुराना राज बाहर आने लगा। रवि और गिरीश कॉलेज के दोस्त थे, बाद में मिलकर कंपनी शुरू की। लेकिन गिरीश ने धोखा दिया, पैसे हड़प लिए, रवि को बर्बाद करके गायब हो गया। यह अनन्या के जन्म से भी पहले की बात थी। रवि टूट गए, यह बात किसी को नहीं बताई। अब अनन्या को समझ आया—गिरीश के पास उसके पिता को फंसाने का पुराना मकसद था।
डायरी में एक और राज था—तीन साल पुरानी अखबार की कटिंग। एक हिट एंड रन एक्सीडेंट, जिसमें तेज रफ्तार सेडान ने एक जज की गाड़ी को टक्कर मारी थी—तारीख, जगह वही थी, जब जस्टिस सिन्हा अपाहिज हुए थे। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था—”आज सालों बाद गिरीश मिला, बहुत अमीर हो गया है, काले रंग की विदेशी सेडान चला रहा है, बिल्कुल वैसी जैसे एक्सीडेंट वाली गाड़ी थी। भगवान करे मेरा शक गलत हो।”
अनन्या के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। गिरीश ही वो इंसान था जिसने जस्टिस सिन्हा को अपाहिज बनाया और रवि शर्मा को फंसाया, ताकि अगर रवि कभी मुंह खोले, तो कोई उसकी बात पर यकीन न करे।
अब अनन्या के हाथ में सिर्फ पिता की बेगुनाही का सबूत नहीं था, बल्कि जस्टिस सिन्हा के मुजरिम का नाम भी था। यही था वह राज जो एक अपाहिज जिस्म में जान डाल सकता था।
अगली सुबह, कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले, अनन्या किसी तरह जज के चेंबर में पहुंच गई। जस्टिस सिन्हा उसे डांटने को तैयार थे, लेकिन अनन्या ने शांति से तस्वीर, डायरी के पन्ने और अखबार की कटिंग उनकी मेज पर रख दी। “जज साहब, मैं आपसे अपने पिता के लिए भीख मांगने नहीं आई हूं। मैं आपको आपके मुजरिम का नाम बताने आई हूं।”
जस्टिस सिन्हा ने हैरानी से कागज देखे। तस्वीर में रवि के साथ गिरीश, डायरी के पन्ने, अखबार की कटिंग—सब देख उनका चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा शरीर कांपने लगा। अनन्या ने कहा, “जिस गिरीश की गवाही पर आप मेरे पिता को सजा देने वाले हैं, वही वो इंसान है जिसने तीन साल पहले आपको टक्कर मारी थी।”
यह सुनते ही जस्टिस सिन्हा के अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा। सालों से दबा गुस्सा, दर्द, नफरत, सदमा—सब बाहर आ गया। डॉक्टरों ने हमेशा कहा था—चोट जितनी शारीरिक है, उससे ज्यादा मानसिक सदमे की वजह से गंभीर है। आज जब सदमे की वजह सामने आई, उनके दिमाग के हिस्सों में हरकत हुई, जो सालों से सोए थे। उन्होंने व्हीलचेयर के हैंडल को जोर से पकड़ा, उंगलियां सफेद पड़ गईं।
और फिर वह हुआ जिसे चमत्कार कहते हैं। उनके दाहिने पैर में सालों से बेजान मांस के टुकड़े में हल्की हरकत हुई, एक झनझनाहट महसूस हुई। वह हांफ रहे थे, अविश्वास से टांगों की तरफ देखा। कोर्ट रूम में सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब जस्टिस सिन्हा अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखों में अजीब सी आग थी।
उन्होंने कांपती आवाज में कहा—”आज का फैसला मुल्तवी किया जाता है।” उन्होंने पुलिस को आदेश दिया—गिरीश को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, उसकी तीन साल पुरानी काली सेडान गाड़ी फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त की जाए।
पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। पुलिस की जांच में गाड़ी के बंपर से तीन साल पुराने खरोंचों के निशान मिले, जिनका पेंट जज साहब की गाड़ी से मैच कर गया। दबाव में गिरीश टूट गया, अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना—उस रात नशे में उसी ने जज साहब को टक्कर मारी थी और रवि शर्मा को फंसाया, क्योंकि डर था कि रवि उसका राज जानता है।
अगले दिन उसी कोर्ट रूम में जस्टिस आनंद सिन्हा ने कांपते हाथों से फैसला सुनाया—रवि शर्मा को बाइज्जत बरी किया जाता है। जैसे ही रवि कटघरे से बाहर आया, अनन्या दौड़कर उससे लिपट गई। बाप-बेटी के आंसुओं ने पूरे कोर्ट को भावुक कर दिया।
लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। सदमे के समाधान ने जस्टिस सिन्हा के शरीर पर जादू की तरह काम किया। उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे फिजियोथेरपिस्ट की मदद ली। अब उनके अंदर जीने की नई इच्छा जाग चुकी थी। महीनों की मेहनत के बाद, धीरे-धीरे पैरों में जान लौटने लगी।
एक साल बाद, रवि शर्मा वापस लाइब्रेरियन की नौकरी कर रहे थे, सम्मान लौट चुका था। अनन्या अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। वे दोनों आज जस्टिस सिन्हा से मिलने उनके घर आए। जस्टिस सिन्हा ने दरवाजा खुद खोला—व्हीलचेयर पर नहीं, बैसाखी के सहारे, अपने पैरों पर खड़े थे। चेहरे पर अब कड़वाहट नहीं, एक शांत मुस्कान थी।
उन्होंने अनन्या से कहा—”उस दिन तुमने कोर्ट में कहा था कि तुम मुझे चलना सिखा दोगी। तुमने सिर्फ मेरे पैर ही नहीं लौटाए, मुझे फिर से जीना भी सिखाया है। तुमने सिर्फ अपने पिता को नहीं बचाया बेटी, मुझे भी मेरी कैद से आजाद कर दिया है।”
जस्टिस सिन्हा ने फैसला किया—वह अनन्या की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। वह चाहते थे, अनन्या एक वकील बने—क्योंकि जिसमें 15 साल की उम्र में न्याय के लिए इतनी आग हो, वह भविष्य में इंसाफ की सच्ची मशाल बन सकती है।
कहानी की सीख:
एक बेटी का प्यार और विश्वास दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ा होता है। सच्चाई में वह शक्ति है जो ना सिर्फ बेड़ियों को तोड़ सकती है, बल्कि गहरे से गहरे जख्मों को भी भर सकती है। कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए—क्योंकि इंसाफ और चमत्कार अक्सर वहीं होते हैं, जहां हम उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं।
समाप्त
डॉक्टर बहू ने सास को अनपढ़ कहा… पर सास की असली जानकर पैर पकड़ ली फ़िर जो हुआ

सास-बहू, अहंकार और इंसानियत की सीख
जयपुर शहर में सुनीता जी का घर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उनके इकलौते बेटे रोहित की शादी थी, और पूरा घर खुशियों से भरा था। रिश्तेदार, दोस्त, सब डीजे की धुन पर नाच रहे थे। सुनीता जी का बेटा रोहित पढ़ा-लिखा और समझदार था, और आज उसकी शादी सिया से हो रही थी। सिया अपने माता-पिता की इकलौती बेटी और एक होनहार डॉक्टर थी। उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई पर खूब मेहनत और पैसा लगाया था, और सिया ने भी उन्हें गर्वित किया था। लेकिन सिया के दिल में अपनी नौकरी, डिग्री और हैसियत का घमंड भी आ गया था। वह सोचती थी, “मैंने इतनी मेहनत की है, इतना कमाया है, मेरे सामने कौन टिक सकता है?”
शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। सिया अपनी नई जिंदगी शुरू करने ससुराल आई, लेकिन उसके दिल में वही घमंड था जो उसे हर किसी को छोटा दिखाने पर मजबूर करता था। रोहित का परिवार छोटा था—सुनीता जी, उनकी बेटी नेहा और अब नई बहू सिया। रोहित के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 15 साल का था। हार्ट अटैक ने उन्हें छीन लिया, और तब से सुनीता जी ने अकेले ही अपने बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया।
शादी के अगले दिन घर में नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी। सुनीता जी ने अपनी बेटी नेहा को बुलाया और कहा, “बिटिया, जाओ अपनी भाभी को बोलो कि मेहमान हॉल में इकट्ठा हो गए हैं। उन्हें अच्छे से सजधज कर आने को कहो।” नेहा उत्साह से सिया के कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी सिया तेज कदमों से बाहर निकल आई। मेहमानों की नजरें उस पर टिक गईं और सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। नई बहू जिसे लहंगे, साड़ी और गहनों में सजना चाहिए था, वो जींस और टॉप में थी।
मेहमान आपस में खुसरफुसर करने लगे, “अरे ये क्या? नई बहू तो बिल्कुल अलग अंदाज में है।”
सुनीता जी ने धीरे से कहा, “बेटा, जाओ साड़ी पहनकर आओ। मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आए हैं।”
लेकिन सिया का जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने तीखे लहजे में कहा, “मां जी, मुझे क्या समझा रही हैं? मैं पढ़ी-लिखी हूं। कोई आप जैसी गंवार नहीं जो साड़ी में लिपटी रहूं। इतनी गर्मी में 5 मीटर की साड़ी मैं नहीं लपेट सकती। वैसे भी सुना है आप किसी छोटे से गांव की हैं, तभी आपकी सोच इतनी पुरानी है। हम मॉडल लोग जींस और टॉप पहनते हैं।”
सुनीता जी का चेहरा लाल हो गया। मेहमानों के सामने उनकी बहू ने उनकी ऐसी बेइज्जती की थी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वह चुप रहीं। उन्होंने मेहमानों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, “अरे गर्मी बहुत है ना, इसलिए बहू ने कपड़े बदल लिए। चलो कोई बात नहीं, रस्म ऐसे ही कर लेते हैं।”
उनका दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी भावनाओं को दबा लिया।
अगले दिन सुबह पहली रसोई की रस्म थी। नेहा उत्साहित होकर सिया के कमरे में गई और मुस्कुराते हुए बोली, “भाभी, मां ने आपको किचन में बुलाया है। आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। और हां, रस्म के बाद मेरे लिए गरमागरम पकोड़े और चाय बना देना। मेरी सहेलियां भी आएंगी, उन्हें भी आपके हाथ का खाना खिलाने का मन है।”
नेहा की मासूम बात सुनकर सिया भड़क उठी। उसने सख्त लहजे में कहा, “ननद जी, जिसे चाय-पकोड़े खाने हैं, वह अपने हाथ-पैर चलाए और बनाएं। मैं तुम्हारे घर शादी करके आई हूं, कोई नौकरानी नहीं बनी। मेरे सामने ऑर्डर देने की हिम्मत मत करना। यह मत सोचो कि भाभी आई है तो घर में रेस्टोरेंट खुल गया। मैं सिर्फ रस्म निभाने के लिए किचन में जाऊंगी। वैसे भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ी-लिखी हूं। मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है, तुमने मुश्किल से ग्रेजुएशन किया होगा, वो भी शायद नकली डिग्री लेकर। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूं, तुम्हारी तरह बेकार नहीं। अगर तुम्हें कोई छोटी-मोटी नौकरी भी मिल जाए तो ₹4000 से ज्यादा नहीं कमा पाओगी। यह घर तो मेरे और रोहित के पैसों से ही चलेगा।”
नेहा के दिल में सिया की बातें तीर की तरह चुभ गईं। उसकी आंखें छलक आईं, लेकिन वह चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो। वह आंसुओं को छुपाते हुए अपने कमरे में चली गई।
इधर सिया रसोई में पहुंची। सुनीता जी ने पहले से ही खीर बनाकर रखी थी। सिया ने बस कड़छी से खीर को हिलाया, थोड़ी चीनी और मेवे डाले और रस्म पूरी कर दी। जब वह मेहमानों को खीर परोसने गई तो उसने फिर सबके सामने चिल्लाकर कहा, “मां जी, मैं आज के जमाने की मॉडल लड़की हूं।”
रस्म के दौरान बड़ी मामी ने सिया को चांदी की अंगूठी दी। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, “मामी जी, हमारे यहां तो सिर्फ गोल्ड और डायमंड पहना जाता है। चांदी की अंगूठी तो नौकरानियां पहनती हैं।”
बुआ जी ने उसे ₹1000 का नोट दिया तो उसने ताना मारा, “बुआ जी, ₹1000 में क्या होगा? हमारे यहां तो नौकरों को भी इतना नहीं दिया जाता। खैर, कोई बात नहीं। मेरे पापा ने सबके लिए लिफाफे दिए हैं।”
वो कमरे से लिफाफे लाई और मेहमानों को बांटने लगी, “यह लीजिए बुआ जी ₹1100, और यह मामी जी आपके लिए। हमारा रुतबा ही कुछ और है। हम छोटे-मोटे जॉब नहीं करते, बड़ी कंपनियों और हॉस्पिटल्स में काम करते हैं।”
सुनीता जी ने फिर समझाया, “बेटा, शगुन के लिफाफे तो ठीक है लेकिन बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लो।” लेकिन सिया फिर भड़क गई, “मां जी, आपने मुझे कोई नौकरानी समझ रखा है? इतने लोगों के पैर छूने से मेरी कमर टूट जाएगी। मैं कोई पुराने जमाने की बहू नहीं। मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है, मेरा पैकेज तो आपको पता ही होगा। मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं आपके रिश्तेदारों के पैर दबाऊंगी।”
मेहमानों में खुसरफुसुर तेज हो गई। कोई बोल रहा था, “सुनीता की किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मिली।”
सुनीता जी की आंखें नम थी, लेकिन वह फिर भी चुप रहीं।
सच का खुलासा और बहू का घमंड टूटना
एक दिन सिया का ममेरा भाई पवन विदेश से आया। सिया खुशी से झूम उठी, “भाई, शाम को 5 बजे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रोहित भी साथ आएगा।”
लेकिन पवन सरप्राइज देने के लिए 2 घंटे पहले ही ससुराल पहुंच गया। डोरबेल बजी, नेहा ने दरवाजा खोला। सामने एक स्मार्ट सूट-बूट में सजा शख्स खड़ा था। “जी आप कौन?”
“मैं पवन, सिया का ममेरा भाई, दुबई से आया हूं।” नेहा ने उसे अंदर बुलाया। तभी सुनीता जी किचन से बाहर आईं, “कौन है बिटिया?”
“मां, ये भाभी के भाई हैं।”
पवन ने सुनीता जी को देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर उनके पैर छूने लगा, “मैम, मैं आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था, आप यहां!”
सुनीता जी हैरान थीं, “बेटा, तुम कौन हो?”
पवन ने कहा, “मैम, मैं पवन कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका स्टूडेंट। आपको याद है, मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। अगर आपने मेरी फीस ना भरी होती, किताबें ना दिलाई होती, मुझे फ्री में क्लासेस ना पढ़ाई होती, तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं।”
धीरे-धीरे सुनीता जी को याद आने लगा। उनकी आंखें नम हो गईं।
तभी सिया घर लौटी। उसने देखा कि उसका भाई पवन उसकी सास के पैर छू रहा है और उन्हें “मैम” कह रहा है।
सिया को यकीन नहीं हुआ, “पवन, तुम क्या कह रहे हो? मेरी सास तो अनपढ़ है, ये कोई प्रोफेसर नहीं हो सकती।”
पवन ने गंभीरता से कहा, “गरिमा, तुम गलत हो। ये सुनीता वर्मा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। इन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी जिंदगी बनाई।”
सिया का दिल धड़कने लगा। वो दौड़कर सुनीता जी के कमरे में गई और उनकी अलमारी खोली। वहां उसे ढेर सारी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिले। उसकी आंखें चौंधिया गईं।
वो रोते हुए बोली, “मां जी, अगर आप इतनी पढ़ी-लिखी थीं तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको अनपढ़ समझकर इतना कुछ कहती रही।”
सुनीता जी शांत स्वर में बोलीं, “बेटा, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं वही सुनीता वर्मा हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी। जब रोहित के पिता का देहांत हुआ, तब मुझे अकेले बच्चों को संभालना पड़ा। फिर जब मेरे ससुर जी बीमार हुए, तो मुझे जयपुर आना पड़ा। उनकी सेवा के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने ट्यूशन पढ़ाए, बच्चों को संभाला और हर मुश्किल का सामना किया।”
उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। कुछ स्टूडेंट्स सुनीता जी को टीचर्स डे की बधाई देने आए थे। वे मिठाइयां, बुके और साड़ियां लाए थे। एक स्टूडेंट बोला, “मैम, आपके बिना मैं गोल्ड मेडल ना जीत पाता।”
सिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस सास को वह अनपढ़ समझती थी, उन्हें लोग इतना सम्मान दे रहे थे।
तभी पवन ने सुनीता जी से कहा, “मैम, मैं आपकी बेटी नेहा का हाथ मांगना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने उसे अपने संस्कार दिए होंगे।”
सुनीता जी ने खुशी से हां कर दी।
सिया का सिर शर्म से झुक गया। वो रोते हुए सुनीता जी के पास गई और बोली, “मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इतना बुरा भला कहा।”
सुनीता जी ने उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, “बेटा, कभी किसी को कम मत समझना। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है। तुमने जो किया वह तुम्हारी नादानी थी। अब इसे भूल जाओ और जाओ मेरे स्टूडेंट्स के लिए चाय और पकोड़े बनाओ। यही तुम्हारी सजा है।”
सिया मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब कभी अपनी नौकरी या डिग्री का घमंड नहीं करेगी और घर के काम में सुनीता जी की मदद करेगी।
सीख:
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। नौकरी करना, पढ़ा-लिखा होना या पैसा कमाना हमें दूसरों से ऊपर नहीं बनाता।
बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना, घर के काम में हाथ बटाना और अपने अहंकार को छोड़ना ही हमें सच्चा इंसान बनाता है।
सुनीता जी ने अपनी काबिलियत को कभी घमंड नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और यही संस्कार नेहा को एक अच्छा जीवन साथी दिलाने में काम आए।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सुनीता जी ने सिया को माफ करके सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
फिर मिलते हैं एक और दिल को छूने वाली कहानी के साथ।
जय हिंद!
News
लुंगी पहनकर थाने पहुंचा ये आदमी… और 5 मिनट में दरोगा सस्पेंड! | असली SP की सच्ची कहानी
लुंगी पहनकर थाने पहुंचा ये आदमी… और 5 मिनट में दरोगा सस्पेंड! | असली SP की सच्ची कहानी . ….
अस्पताल में लोगों को लूटा जा रहा था, फिर डीएम ने सबक सिखाया।
अस्पताल में लोगों को लूटा जा रहा था, फिर डीएम ने सबक सिखाया। . . जिले की सबसे बड़ी अधिकारी,…
IPS मैडम को आम लड़की समझ कर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा फिर जो हुआ
IPS मैडम को आम लड़की समझ कर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा फिर जो हुआ . . सुबह का समय था।…
“जब वर्दी वालों ने SDM प्रिया वर्मा को ही सिखाने चले सबक | सच्ची घटना
“जब वर्दी वालों ने SDM प्रिया वर्मा को ही सिखाने चले सबक | सच्ची घटना . . बारिश की बूंदें…
IPS मैडम ने की एक 14 वर्ष के लड़के से शादी, आख़िर क्यों..? फिर अगले ही दिन जो हुआ “…
IPS मैडम ने की एक 14 वर्ष के लड़के से शादी, आख़िर क्यों..? फिर अगले ही दिन जो हुआ “……
SP मैडम के पिता को मार रहे थे पुलिस वाले- फिर एसपी मैडम ने जो किया सबको हैरान कर दिया…सच्ची घटना
SP मैडम के पिता को मार रहे थे पुलिस वाले- फिर एसपी मैडम ने जो किया सबको हैरान कर दिया…सच्ची…
End of content
No more pages to load