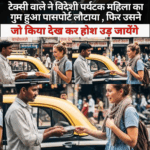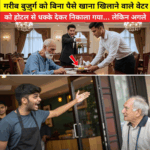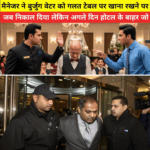मैकेनिक ने 24 घंटा काम करके फौजी ट्रक ठीक किया , और पैसे भी नहीं लिए , फिर जब फौजी कुछ माह बाद
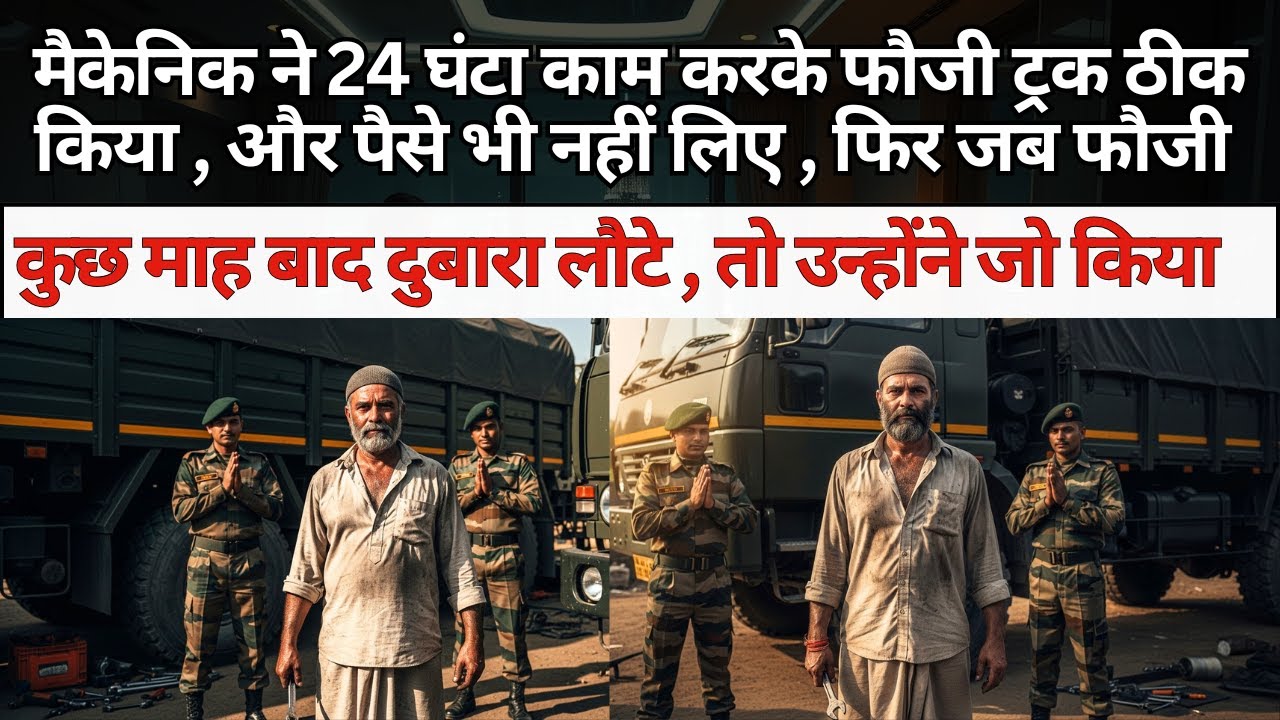
ऊँचे-ऊँचे देवदारों की कतारें, उनके बीच से कटती एक साँप-सी लहराती सड़क, हवा में नमक जैसी चुभन लिए बर्फ की किरचें और दूर ऊँचाई पर भोर से पहले का नीला अँधेरा—जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 44) उस सुबह भी एक धीर गंभीर लय में साँस ले रहा था। यही सड़क सर्दियों में जीवनरेखा भी थी और अनिश्चित मौत का ख़तरा भी। इसी चुनौती भरे परिदृश्य में एक छोटा-सा टिन का खोखा—’रफ़ीक ऑटॉवर्क्स – 24 घंटे सेवा’—मानो किसी बुझते हुए दीये की लौ बनकर ठिठुरते सफ़रियों को गर्माहट देता था। यह कहानी उसी दीये, उसके रखवाले रफ़ीक अहमद, उसके सपने देखने वाले बेटे इरफ़ान और भारतीय सेना के उन जाँबाज़ों की है जिनके लिए कर्तव्य सांस लेने से भी बड़ा सच था।
अध्याय 1: वीराने का धड़कता धड़कनघर
रफ़ीक अहमद लगभग चालीस का था। गेहुआँ रंग, ठंडी हवा से फटती त्वचा, आँखों में अजीब-सी दर्पविहीन चमक—जिसे देखने पर लगता मानो किसी शांत झरने ने पत्थरों को चूम-चूम कर खुद को साफ़ कर लिया हो। उसकी दुकान के पीछे कच्चे पत्थरों और लकड़ी की बल्लियों से बना एक छोटा-सा कमरा था—यही रसोई, यही शयन, यही बैठक। पत्नी ज़रीना की धीमी, समझदार मुस्कान और बारह साल का बेटा इरफ़ान—यही उसका परिवार, यही उसकी दुनिया।
इरफ़ान की Pupils में एक अलग आग थी। जब भी सड़क से हरे रंग के ‘स्टैलियन’ ट्रक या बख़्तरबंद गाड़ियाँ गरजती हुई निकलतीं, वह साँस रोककर उन्हें देखता। उनके पीछे उड़ती बर्फ या धूल उसकी कल्पना को वर्दी, सलामी, तिरंगे और परेड ग्राउंड के दृश्यों से भर देती। उसकी नोटबुक के पिछले पन्नों पर कई बार उसने अपने नाम के आगे लिखा था—”लेफ़्टिनेंट इरफ़ान अहमद”—और फिर शर्मा कर काट दिया था।
रफ़ीक जानता था बेटा क्या चाहता है। वह चाहता था इरफ़ान पढ़े, आगे बढ़े; पर ठंडी हक़ीक़त यह थी कि इस वीराने में शिक्षण संसाधन उतने ही विरल थे जितनी सर्दियों की धूप। शहर भेजना? किराया, हॉस्टल, फ़ीस—यह सब उसके औज़ारों के जंग लगे बक्से और कभी-कभार मिलने वाले ग्राहकों की जेब से बाहर था। यही द्वंद्व उसका स्थायी मौन था।
अध्याय 2: सेवा का संकल्प
इस सुनसान स्ट्रेच पर उसकी दुकान एक अनकही प्रतिज्ञा थी। कोई भी—ट्रक ड्राइवर, टैक्सी वाले, पर्यटक, या सेना का क़ाफ़िला—यदि अटक जाए, रफ़ीक ‘ना’ कहना जानता ही नहीं था। रात, बर्फ़, तूफ़ान, बिजली कड़कना—इन सबका उसके “हाँ उस्ताद… अभी देखता हूँ” पर कोई असर न होता। फ़ौजी आते तो वह पहले चाय का कड़छा चढ़ाता, फिर औज़ार उठाता। पैसे लेने में झिझक, मुस्कान में अपनापन। वह कहता, “आप लोग सरहद बचाते हो, मैं आपकी राह बचा लूँ तो क्या कम?”
कई जवान उसे “उस्ताद” कहकर संबोधित करते और इरफ़ान को बुला लेते—“आओ छोटू, गियर बॉक्स सम्हालो।” इरफ़ान फिर गर्व से सीना चौड़ा कर टॉर्च पकड़ खड़ा हो जाता।
अध्याय 3: दिसंबर की क्रूरतम रात
दिसंबर का आख़िरी सप्ताह। तापमान शून्य से नीचे फिसल चुका था। हवा अब केवल चल नहीं रही थी; वह चाबुक बनकर कट रही थी। शाम ढल चुकी थी। बादल दबे पाँव पहाड़ियों पर चढ़ आए थे। रफ़ीक शटर आधा खींच ही रहा था कि पीछे से बर्फ़ पर किसी के पैर फिसलने की हड़बड़ी भरी आवाज़ आई।
एक जवान—चेहरे पर थकान, सांस धौंकनी—दरवाज़े पर लड़खड़ाता आ खड़ा हुआ। “उस्ताद… दो किलोमीटर आगे मोड़ पर ट्रक बंद पड़ गया… जरूरी लोड है…” शब्दों के बीच उसकी साँसें भाप बनकर उड़ रही थीं।
रफ़ीक ने बिना प्रश्न किए औज़ारों का लोहे का बक्सा उठाया, कंधे पर गंदा, गाढ़े तेल से भीगा कपड़ा लटकाया और बोला, “चलो।”
अध्याय 4: संकट का स्टैलियन
घुमावदार मोड़ पर पहुंचते ही आवाज़ों ने हवा को चीर दिया—“आ गए?”, “जल्दी देखो!”—और टॉर्चों की पीली प्रकाश-धारियों के बीच भारतीय सेना का विशाल ‘स्टैलियन’ ट्रक ठंड से जकड़ा एक घायल हाथी लग रहा था। पास खड़े जवान मोमजामे में भी काँप रहे थे।
एक गंभीर, दबा हुआ स्वर पास आया—“मैं सूबेदार बलविंदर सिंह।” उनकी दाढ़ी पर जमी बर्फ़ के रेशे छोटे क्रिस्टल-से चमक रहे थे। आँखों में तत्परता, माथे पर चिंता की महीन सिलवटें।
“नाम?”
“रफ़ीक… उस्ताद बोल लेते सब।”
सूबेदार का उत्तर तुरंत स्वर में बदल गया, “रफ़ीक, इसमें राशन, दवाइयाँ, विंटर गियर है। तड़के से पहले श्रीनगर की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुँचना अनिवार्य है। वायरलेस सिग्नल नहीं जा रहा। तुम उम्मीद हो। कर लोगे?”
“खोलकर देखता हूँ, साहब।”
अध्याय 5: ठंडी धातु, गरम इरादा
रफ़ीक ने बोनट उठाया। टॉर्च की रोशनी में वाष्पीकृत डीज़ल और जल वाष्प ने एक धुंध-सा घेरा बनाया। उसने हाथ डाला—ठंडी धातु ने नसों में सुन्नता भर दी। आधे घंटे की टटोल, चाबी कस-ढीली करने के बाद वह बाहर निकला। “क्लच प्रेशर पाइप फटा है, गियर बॉक्स का ऑयल सील लीक—ऑयल निकलता रहेगा तो गियर जाम मारेंगे। सामान पूरा नहीं है मेरे पास। जुगाड़ करना पड़ेगा—पुरानी हाइड्रोलिक पाइप को काटकर क्लैंप से सेट कर दूँगा। सील की जगह रबर फैब्रिक की डल्ली बना दूँगा। वक़्त लगेगा।”
“कितना?”
“मौसम साथ दे तो—सात आठ घंटे। पर बर्फ़ बढ़ी तो… कोशिश सुबह से पहले।”
सूबेदार ने आकाश देखा—बर्फ़ की फुहारें अब गुच्छों में बदल रही थीं। “जो चाहिए लो। जवान साथ हैं।”
यही वाक्य उस रात छेड़ी गई अनकही साझेदारी का ‘संक्षिप्त सैन्य आदेश’ था।
अध्याय 6: रात—एक कार्यशाला बनाम युद्धभूमि
उसने ट्रक जेक से उठवाकर रेंगते हुए शरीर नीचे सरकाया। जमीन का हिम मिश्रित पत्थर उसकी पीठ के आर-पार चुभ गया। हवा सीटी मारती, ट्रक के चेसिस से टकराकर वापस उसके गाल पर बर्फ़ की महीन सुइयाँ फेंकती। इरफ़ान चुपके से घर से निकल आया—माँ ने रोकना चाहा, पर उसकी आँखों की प्रार्थना देखकर चुप रह गई।
ज़रीना ने मिट्टी के तंदूर में अंगारों को फूँक दी, उबलते पानी में काली चाय, दालचीनी, इलायची डाली। धुएँ में गीली लकड़ी की गंध, चाय की महक घुलकर जवानों के थरथराते शरीरों तक पहुँची। उसने ऊँची आवाज़ लगाई, “भाई जी, पहले गरम चाय—फिर काम। अंदर आ जाइए—हड्डियाँ जम जाएँगी!”
रफ़ीक ने भीतर से आवाज़ दी, “आप लोग जाइए, मैं हूँ नीचे।”
उसने एक पुराना फटा ट्यूब निकाला, कैंची से धारदार काट बनाया, गोद में रखी टॉर्च को इरफ़ान ने नीचे झुका रखा:
“अब्बू, ठंड लग रही?”
“हाथ चल रहे हैं ना—यही काफी।”
“मैं बड़ा होकर वही बनूंगा, जिनके लिए तुम काम कर रहे।”
“पहले पढ़ाई… फिर वर्दी… क्रम ज़रूरी है।”
उनके बीच की वह ठंडी अंधेरी जगह किसी कक्षा का रूप ले चुकी थी—मशाल टॉर्च थी, पाठ राष्ट्रधर्म।
अध्याय 7: स्वाभिमान की गरम भट्ठी
रात गहरी—बर्फ़ मोटी। रफ़ीक के हाथ की उँगलियों की पोरें फट कर हल्का-हल्का खून रंग छोड़ने लगीं, जो तुरंत जमकर गाढ़ा कत्थई छल्ला बन जाता। सूबेदार कई बार बोले, “उस्ताद, थोड़ा रुक जाओ, हाथ सेंको।”
हर बार जवाब एक मुस्कान, “साहब, आप लोग चौबीस घंटे ड्यूटी—मैं एक रात नहीं जागूँ? काम रोका तो शरीर मान जाएगा।”
एक जवान ने दबे स्वर में कहा, “सर, ऐसा आदमी पोस्टिंग मिल जाए हमारे साथ तो…”
सूबेदार ने धीरे उत्तर दिया, “ऐसे लोग किसी पोस्ट पर नहीं—दिल में पोस्ट होते हैं।”
उनकी आँखों ने उसी क्षण भविष्य में लौटकर कुछ निर्णय ले लिया था जिसे शब्दों की ज़रूरत न थी।
अध्याय 8: प्रात की पहली रेखा और स्टार्ट की गर्जना
घड़ी ने लगभग पाँच का घंटा जपा। पूर्व में हल्की चाँदी चढ़ने लगी। रफ़ीक ने अंतिम बार अस्थायी क्लैंप को कसकर हथेली से थपथपा दिया, गियर लीवर की मूवमेंट टेस्ट की, फिर—कसावट से भरी थकी आवाज़, “साहब… कोशिश हो गई… स्टार्ट मारिए।”
सूबेदार ने केबिन में चढ़कर इग्निशन घुमाया। ग्लो प्लग के बाद इंजन ने एक भारी कराह भरी, फिर धक्का लगा, और अगले ही पल गहरी, भरोसेमंद गरज। धुएँ की लकीर ने आसमान में जैसे विजय ध्वज खींच दिया। जवानों ने एक स्वर में—“भारत माता की जय!”—गूंज पहाड़ों पर टकराकर लौटी। दो ने आगे बढ़कर रफ़ीक को कंधों पर उठा लिया। वह झेंपता, “अरे अरे… ज़मीन पर रखो… मेरा क्या।”
सूबेदार नीचे आए, दस्ताने उतारकर नंगे हाथ से उसका हाथ थामा—“मूल्य?”
रफ़ीक ने दोनों हथेलियाँ पीछे कर लीं, “यह सवाल मत पूछिए। यह दुकान पैसा कमाने का अड्डा नहीं—रास्ता खुला रखने का इरादा है। आपकी दुआ लगी रही तो बच्चा पढ़ जाएगा—वही पर्याप्त।”
सूबेदार की आँखें क्षण भर भीग सी गईं। उन्होंने बस इतना कहा, “तुम सिर्फ मैकेनिक नहीं—राष्ट्र के सिपाही हो, बिना वर्दी।”
ट्रक प्रस्थान कर गया। इरफ़ान दूर तक उसे जाता देखता रहा—बर्फ में टायर के निशान रह गए—मानो भाग्य ने राह में कोई अदृश्य पगडंडी छोड़ दी हो।
अध्याय 9: मौन ऋतु और प्रतीक्षा
चार महीने बीत गए। बर्फ़ की चादर हटने लगी, पहाड़ी ढालों पर कोमल हरे पुच्छ उग आए। जीवन ने गति पकड़ी। पर इरफ़ान अक्सर पूछ बैठता, “अब्बू, वो सूबेदार अंकल फिर आएंगे?”
“आएंगे—फ़ौजी वादा निभाते हैं,” रफ़ीक साधारण विश्वास से कह देता पर भीतर हल्का-सा संशय रह जाता—फौजियों की पोस्टिंग अनिश्चित होती है।
ज़रीना ने एक दिन कहा, “तुमने उनसे कुछ मांगा नहीं।”
“माँग ली होती तो वह रात काम सौदे में बदल जाती—और सौदा सेवा पर पर्दा डाल देता,” रफ़ीक ने उत्तर दिया।
अध्याय 10: “हम चाय का कर्ज उतारने आए हैं”
एक चमकीली दोपहिर, सड़क पर धूल से ज्यादा प्रकाश था। दूर इंजन की आवाज़ ने हवा को पहले से चेताया। स्टैलियन फिर मुड़ा और दुकान के सामने धीमे से रुका। इरफ़ान का चेहरा खिल उठा। रफ़ीक औज़ार फेंककर बाहर भागा, “आओ साहब! आज तो मौसम ने भी सलाम ठोका।”
सूबेदार बलविंदर उतरे—चेहरे पर इस बार एक शांति थी, मानो कोई निर्णय आकार ले चुका हो। “उस्ताद, आज हम चाय पीने नहीं—चाय का कर्ज उतारने आए हैं।”
रफ़ीक चौंका। इरफ़ान स्कूल की थैली लेकर दरवाज़े पर आ लगा। सूबेदार ने उसे पास बुलाया, सिर पर हथेली रखी—“नाम?”
“इरफ़ान।”
“बड़े होकर?”
“फौजी।”
“शाबाश।”
उन्होंने पीछे से एक प्लास्टिक कवर में रखी फ़ाइल निकाली और रफ़ीक को थमा दी।
“यह?”
“आर्मी पब्लिक स्कूल, जम्मू—एडमिशन डॉक्युमेंट। प्रिंसिपल से बात हो गई। हॉस्टल, फ़ीस, किताबें, यूनिफॉर्म—सब कुछ यूनिट की जिम्मेदारी। यह तुम्हारे त्याग की कीमत नहीं—यह उस भावना का सम्मान है।”
रफ़ीक को लगा जैसे समय थम गया। आँखें धुंध से भर आईं। ज़रीना दरवाज़े पर थाली लिए खड़ी रह गई—थाली हल्की लड़खड़ा गई। “साहब… मैं… हम…” शब्द बिखर गए।
“यह एहसान नहीं,” सूबेदार धीरे बोले। “देश के प्रहरी का परिवार देश का परिवार। तुमने कहा था तुमने फर्ज निभाया—आज हम अपना निभा रहे।”
इरफ़ान का छोटा शरीर सूबेदार की कमर से लिपट गया। पल का मौन सबका सामूहिक प्रण बन गया।
अध्याय 11: परिवर्तन के पगचिह्न
अगले हफ़्तों में कागज़ी औपचारिकताएँ हुईं। पहली बार इरफ़ान ने सही साइज़ की ढेरों किताबें एक साथ देखीं तो आँखें चमक गईं। हॉस्टल के पहले दिन वह अनकहे डर से भरा था। रफ़ीक ने उसे समझाया, “सीना तना रख—याद रख, पढ़ाई भी सेवा की पहली पगडंडी है।”
सूबेदार ने उसे ओरिएंटेशन के दौरान गेट के बाहर सलाम झाड़ते हुए कहा—“यह तुम्हारी पहली पोस्टिंग मान लो—कड़ी लेकिन गौरवपूर्ण।”
दिन दौड़ पड़े: मॉर्निंग फ़ॉल-इन, पीटी, क्लास, लाइब्रेरी, मित्र, प्रतियोगिताएँ। इरफ़ान ने मैथ में कमजोरियों को दुरुस्त किया, अंग्रेज़ी उच्चारण सुधारा—रात को ‘मोटिवेशन’ बोर्ड पर अक्सर लिखता—“अब्बू की हथेली के छाले—मेरी प्रेरणा।”
अध्याय 12: परीक्षा, धैर्य और एनडीए
बारहवीं के बाद की साँस रोकी हुई प्रतीक्षा—एनडीए की लिखित परीक्षा निकली। अब SSB (सर्विस सेलेक्शन बोर्ड)। पाँच दिन की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, समूहिक कसौटियाँ।
Group obstacle race में जब एक ऊँची दीवार पर उसकी टीम अटक गई, इरफ़ान को पल भर को अपने अब्बू का ट्रक के नीचे तने हाथ वाला दृश्य याद आया—“आराम नहीं—काम।” वह सबसे पहले कंधा देकर साथियों को ऊपर कराया। Conference दिन अंतिम अधिकारी ने पूछा, “तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा?”
उसने उत्तर दिया, “एक साधारण मैकेनिक—मेरे पिता—जिन्होंने मुझे सिखाया कि देश सेवा का पहला पाठ स्वार्थ छोड़ने से शुरू होता है।”
सिफारिश पत्र आया—चयनित।
अध्याय 13: दीक्षांत और वह सलामी
NDA, फिर IMA. ड्रिल स्क्वाड, राइफ़ल स्ट्रिपिंग, रात्री नेविगेशन, सामरिक नक्शे, फ्रैक्चर ब्लिस्टर, पसीने से भिगोई कैमो जैकेट—सबने उसे गढ़ा। Passing Out Parade के दिन धूप तिरछी सुनहरी थी। परेड ग्राउंड पर टैक्टिकल ढंग से घूमती बैण्ड की स्वर लहरियाँ हवा को भर रहीं थीं। ज़रीना सिर पर दुपट्टा सम्हाले आसमान और बेटे दोनों को देखती—कौन ज्यादा चमक रहा, तय नहीं कर पा रही थी।
रफ़ीक ने पहली बार सही फिटिंग का सूट पहना—कंधे पर अभी भी ग्रीस के दाग की स्मृति पड़ी थी मानो पहचान के लिए।
कमांडेंट ने “आप अपने प्लेटून कमांडर से सलामी स्वीकारिए” कहा। तब लेफ़्टिनेंट इरफ़ान अहमद जैसे आगे बढ़े, सूबेदार बलविंदर सिंह—जो अब पदोन्नत होकर सूबेदार मेजर थे और अतिथि के रूप में उपस्थित—ने खड़े होकर कड़क सलामी ठोकी, “जय हिंद, सर!”
इरफ़ान की पलकों के पीछे वह रात, वह टूटता क्लच पाइप, वह टॉर्च की किरण, वह चाय की भाप—सब एक फ़िल्म बन चली। उसने सलामी लौटाई—उस सलामी में पुत्र धर्म, गुरुदक्षिणा, और राष्ट्रप्रेम की संयुक्त परिक्रमा थी।
अध्याय 14: वही दुकान, नई रोशनी
कुछ वर्षों बाद भी ‘रफ़ीक ऑटॉवर्क्स’ के टिन के ऊपर वही धुंधले अक्षर थे। पर अब भीतर टँगी एक फ़्रेम में लेफ़्टिनेंट (अब कैप्टन) इरफ़ान अहमद की फोटो थी, नीचे छोटे अक्षरों में—“हर इंजन को चलाने में जो हाथ लगे, वही देश के इंजन को चला रहे।”
जब भी नया काफ़िला रुकता, जवान नए होकर भी उस तस्वीर की ओर देख मुस्कुरा देते—“उस्ताद, यह आपके बेटे?”
रफ़ीक आँखें सिकोड़ लेते—गर्व छिपाते, “हाँ, वही—चाय लाऊँ?”
ज़रीना अब बूढ़ी आँखों से दूर सड़क को कम और लोगों के चेहरे ज्यादा पढ़ती। उनकी मुस्कान में संतोष की महीन झुर्रियाँ थीं।
अध्याय 15: एक और रात—सेवा अनवरत
एक बार फिर अचानक शाम को एक सिविल एम्बुलेंस के ब्रेक फेल होने के कारण मोड़ पर भय पैदा हो गया। रफ़ीक ने दौड़कर पत्थरों की वेज लगा कर उसे रोका। अंदर एक गर्भवती महिला, जो कश्मीर से जम्मू रेफ़र हो रही थी। उसने चटपट ब्रेक लाइन में हवा की लीक ढूँढ़ कर अस्थायी मरम्मत की। कोई मीडिया नहीं, कोई ताली नहीं—सिर्फ चालक का देर तक झुकना और जाने से पहले उसका कहना, “आपके बेटे जैसे लोग सरहद बचाते हैं—आप सड़क बचाते हैं।”
रात को रफ़ीक ने आसमान देखा—तारे किसी अदृश्य ड्यूटी रोस्टर की तरह टंगे थे। वह बुदबुदाया, “जिसे जहाँ पोस्ट किया वहीँ चौकस रहे—यही नियम।”
अंतिम अध्याय: देश सेवा का विस्तारित अर्थ
यह कहानी सिर्फ एक मैकेनिक के त्याग और सेना की कृतज्ञता की गाथा नहीं—यह उस सामाजिक ताने-बाने की पुनर्स्मृति है जहाँ राष्ट्रप्रेम पद, वेतन, या वर्दी की परिभाषा से परे है।
रफ़ीक ने सिखाया—कर्तव्य छोटे-बड़े नहीं, केवल निभाए या त्यागे जाते हैं। सूबेदार बलविंदर और उनकी टुकड़ी ने दिखाया—भारतीय सेना लॉजिस्टिक्स और हथियारों की शक्ति मात्र नहीं, स्मृति और संबंधों की भी संरक्षक है। इरफ़ान का उठता सफ़र दर्शाता है—एक पीढ़ी का स्वाभिमानी त्याग अगली पीढ़ी की संरचित संभावना बन सकता है, यदि संस्थाएँ हाथ थाम लें।
और वह दुकान आज भी कहती है—
“देश प्रेम कभी किसी वर्दी का मोहताज नहीं होता;
एक औज़ार पकड़े हाथ और सलामी ठोकते हाथ—दोनों यदि निस्वार्थ हैं तो समान पवित्र हैं।”
उपसंहार (आपके मन के लिए बीज)
जब कभी आप किसी अनजान की सरल मदद करें और बदले में ‘कुछ नहीं चाहिए’ कह दें, तो समझिए—आपने राष्ट्रनिर्माण की अदृश्य नींव में एक ईंट रख दी।
और यदि आप वर्दी में हैं—किसी रफ़ीक को न भूलिए—क्योंकि उसकी दी हुई चाय में सिर्फ पत्ती और दूध नहीं, आपकी यात्रा की निरंतरता का मौन संकल्प घुला होता है।
समापन
पर्वत अब भी वहीं हैं, बर्फ़ अब भी गिरती है, स्टैलियन अब भी गरजते हैं, पर उस वीरान मोड़ पर एक मामूली-सा साइनबोर्ड अब इतिहास की सूक्ष्म परत जैसा लगता है। वहाँ से गुज़रते हुए अगर आप धीमे हों, तो शायद आपको एक क्षण के लिए ग्रीस, चाय, साहस और कृतज्ञता की सम्मिलित सुगंध महसूस हो—वही सुगंध जो किसी भी राष्ट्र की सबसे अमूल्य संपत्ति है।
जय हिंद.
News
गरीब बुजुर्ग को बिना पैसे खाना खिलाने वाले वेटर को होटल से धक्के देकर निकाला गया..
गरीब बुजुर्ग को बिना पैसे खाना खिलाने वाले वेटर को होटल से धक्के देकर निकाला गया.. इंसानियत की असली दौलत…
बस सब्ज़ी मंडी में बुजुर्ग को धक्का देकर गिरा दिया गया.. लेकिन जब उसने अपना नाम बताया
बस सब्ज़ी मंडी में बुजुर्ग को धक्का देकर गिरा दिया गया.. लेकिन जब उसने अपना नाम बताया इज्जत की असली…
मैनेजर ने बुर्जुग वेटर को गलत टेबल पर खाना रखने पर जब निकाल दिया लेकिन अगले दिन होटल के
मैनेजर ने बुर्जुग वेटर को गलत टेबल पर खाना रखने पर जब निकाल दिया लेकिन अगले दिन होटल के इंसानियत…
Govinda Breaks Silence on Divorce Rumors—Is Bollywood’s Iconic Marriage Really Over?
Govinda Breaks Silence on Divorce Rumors—Is Bollywood’s Iconic Marriage Really Over? Bollywood’s beloved “Hero No. 1” Govinda and his wife…
CBI Raids Ambani’s Home: Unmasking Black Money, Political Scandal, and Billionaire Downfall
CBI Raids Ambani’s Home: Unmasking Black Money, Political Scandal, and Billionaire Downfall In a bombshell development that has shaken India’s…
Sister or Suspects? The Sh0cking Twist in Nikki’s Death That Split a Village
Sister or Suspects? The Shocking Twist in Nikki’s Death That Split a Village A small village in Greater Noida is…
End of content
No more pages to load