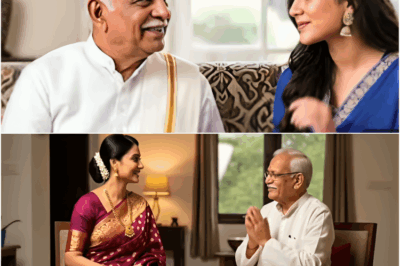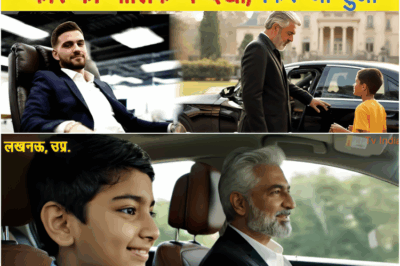बेघर भूखी लड़की ने अपाहिज करोड़पति को एक रूटी के बदले चलना सिखाने का वादा किया
.
.
अंधेरा अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था, और गाँव की कच्ची सड़कें अभी तक भोर की पहली किरणों का इंतज़ार कर रही थीं। उस भीगी हुई सुबह में जहाँ चारों तरफ धुंधे की ओट से पेड़ों की शाखाएँ उभरती थीं, वहीं घरों की छतों पर बैठी चिड़ियाँ अभी चहकने को बेकरार थीं। उसी कच्ची सड़क के किनारे, पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे, एक नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में सफ़ेद टोपी थी, कंधे पर बैग लटका था, और आँखों में एक तरह का जिज्ञासु झुकाव। यह आरोव था, जिसके साहसिक स्वभाव के कारण वह बड़े शहरों के चमचमाते बिजनेस टॉवरों में काम छोड़कर अचानक अपने पैतृक गाँव ‘पावनपुर’ लौट आया था। गाँव के बुज़ुर्ग कहते थे कि दस बीस साल पहले यहाँ बिजली का एक तार भी न था, न मोबाइल नेटवर्क, और सब कुछ वैसा ही था जैसा चाचा-दादी ने बचपन में देखा था। मगर आरोव को वहाँ कुछ और दिखना था—अपने दादा दादी के सपने का शिकन-मुक्त चेहरा।
उसके दादा, रामप्रसाद, गाँव के इकलौते सरकारी स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे। आज से पच्चीस बरस पहले, जब गाँव में पहली बार बिजली आई, तब दादा ने स्कूल की छत पर चार बल्ब लगवाए थे। गाँव के बच्चे पहली बार उस रात अपने स्कूल की चौखट पर खड़े होकर नाचते-गाते बिजली के उजाले को निहारते थे। उसी उत्सव में दादा ने घोषणा की थी कि यह कच्ची सड़क एक दिन पक्की हो जाएगी, गाँव के हर एक कोने तक शिक्षा और स्वास्थ्य की लहर दौड़ेगी। आज-अज से ढाई दशक गुज़र गए, पर सड़क वैसी की वैसी थी, स्कूल की दीवारें धूल-सी जमी थीं, और स्वास्थ्य केंद्र तो दूर, गाँव में औषधालय भी बंद पड़ा था।
आरोव ने कंधे से बैग उतारा। उसमें डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और कुछ पुराने बक्से थे जिनमें—बचपन से दादा के हवाले से इकट्ठा की गई पेन्सिल-स्केल, स्कूल के पुराने नोटबुक के कण-कण, और एक जंग लगी नोकिया की फोन थी। दादा ने हमेशा कहा था, “बेटा, जमीन पर जितना मजबूत इरादा होगा, उतनी ही मजबूती पीछे-पीछे इंतज़ार करेगी।” और इसी वादा के साथ आरोव ने शहर की ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों को पीछे छोड़ दिया था।

गाँव के चौखट पर पहुँचा तो स्मृति लहरों-सी उबरीं—बचपन की उन पगडंडी पर जहाँ वह दादा के हाथ थामे दौड़ता था, माँ के पीछे भागता था जब खेत से ताज़ा मूँगफली और गुड़ लेकर लौटते थे, और दादी के घर के पिछवाड़े में छिपकर मटमैली मिट्टी के खिलौने बनाता था। पर आज सब बदल चुका था—मitti की आँच धीमी हो गई थी, खलिहान सूने पड़े थे, और घरों की छतों से धुँए का कोई निशान नहीं बचा था। गाँव की पुरानी हवेली, जहाँ दादा रहते थे, अब सपाट छतों के नीचे धूल-धूसरित बन्द दीवारें थीं। पोर्च में लगे दो झकझोर देने वाले झूले कांप रहे थे, जैसे सालों से किसी का इंतज़ार कर रहे हों।
उसने जाकी आगे बढ़ाया। सामने स्कूल की बत्ती भी बुझी हुई थी। लोहे का विशाल ताला ताले से भी उतना मजबूत नज़र आता था जितना वर्षों से बिखरते ज़ज़्बातों की याद। दस्तक दी, पर भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। फैसले में दृढ़ता थी कि तालाबन्द खिड़की तोड़कर वह अंदर जाएगा—जैसे बचपन में दादा-बुजुर्ग खामोशी से खोए हुए सपनों को भी बार-बार मुस्कुराना सिखाया करते थे। पर ठीक उसी पल पेड़ की दूसरी ओर से एक हलका-सा रोना कानों में गूंज उठा। आरोव रुक गया और अपनी दिल की धड़कनें थामकर उस आवाज़ की ओर बढ़ा।
वहाँ एक छोटी-सी लड़की बैठी थी, दो हल्की-सी चोटी बाँधे, चेहरे पर निराशा का छाया-सी चढ़ी हुई। उसके हाथ में एक फटी-पुरानी किताब थी और आँखें टुच्चे से झरोखे से बाहर की ओर टिकी थीं। जैसे किसी का इंतज़ार। आरोव ने हौले से पूछा, “बेटी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो?” उस लड़की ने घबराकर मुँह छुपाया, पर फिर भी जरा-सी हिम्मत करके कहा, “मैं कविता हूँ। मैं यहां स्कूल की घंटी सुनने आई थी… पर वो घंटी बजना बंद हो गई।” आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन सीधे दिल में गूंजती थी—एक ऐसा पल जिसमें मासूमियत और दर्द का अजीब सिम्बायोसिस होता है।
आरोव की आँखें भर आईं। भीतर धड़कते खालीपन को उस मासूम चीख़ ने जगाया था। उसने धीरे से कहा, “तुम यहां अकेली कैसे? तुम्हारा घर कहाँ है?” कविता ने जरा तन्मयता से जवाब दिया, “मेरा घर… घर में मेरा कोई नहीं रहता। मेरी माँ खेतों में मजदूरी पर जाती है और दो दिन से लौटकर नहीं आई। मैंने सोचा—यदि स्कूल फिर से खुल जाए तो माँ खुश होंगी।” आरोव के भीतर कोई टूट गया। उसकी माँ, पिता, दादा-नाना—सभी की यादों ने उसे घेर लिया। अपने कंधों पर बैग उठाया, कविता को हाथ पकड़कर खींचा और बोला, “चलिए, तुम्हें घर छोड़ आता हूँ।”
कविता बहते आँसुओं को पोंछकर सर हिलाई। उसी समय आसमान से एक हलका-सा पानी-सा बरसा। महीन बूँदें दोनों के चेहरे छूकर फिसल गईं। कविता मुस्कुराई, उसकी आंखों में उम्मीद का पहला तिलिस्म देखा गया। “देखो,” उसने कहा, “बारिश हो रही है। माँ कहती थी—जब बारिश आती है, तो धरती नहाने चलो।” आरोव ने हँसकर अपनी कंधे की थैली से एक पुराना प्लास्टिक का छाता निकाला, कविता को ताने से ढँक दिया, और दोनों मुलाक़ात की नम आँखों को हीरे-सी चमक दिए हुए, आगे बढ़े।
घरों की कच्ची दीवारें, ताले, हवेली का टूटा दरवाज़ा, सब पीछे छूट रहे थे, और कविता के छोटे कदमों की आहट उनके कदमों को मिलाकर चले जा रही थी। आख़िर एक छोटा-सा झोंपड़ीवाला मकान आया, मुड़ते ही कविता ने रोशनी की एक तरफ़ छुँक दी—जो टूटे हुए बल्ब के बावजूद दहलन का काम देती थी। उसका बेटा, सुनसान गलियों में भूला हुआ, घर पा गया था, और आरोव ने महसूस किया—दूसरों की एक मुस्कान में अपना अस्तित्व भी मुस्कुराकर लौट आता है।
वहाँ कविता की माँ, सुमित्रा, चीख़ते हुए गली में आ रही थी। थके-हारे हाथों में थर्मा, कपड़े गीले, लेकिन चेहरे पर स्वाभाविक ममता की रौशनी थी। दोनों माएँ-बेटियाँ एक-दूसरे को कसकर लाड़े-सा पाकर चिपक गईं। सुमित्रा ने आरोव की ओर देखा—आँखों में कृतज्ञता और हल्की-सी शर्म। दोनों ने कुछ पल तक खामोशी से देखा। फिर सुमित्रा ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और हांफती आवाज़ में कहा, “भैया, मैं… मैं बदलूंगी, मैं हर दिन तुम्हारी मदद करूंगी।” आरोव ने मुस्कुराकर सर हिलाया, “कोई बात नहीं सखी, तुम बस खुश रहो।”
अगले दिन की शुरुआत थी, और आरोव ने तय किया कि जब तक इस स्कूल की घंटी नहीं बजेगी, तब तक वह आराम नहीं करेगा। सुबह-सुबह उसने गाँव के प्रधान, पटेल जी, को पत्र लिख दिया। शाम को पटेल जी आए और बोले, “तू बड़ी दूर से आया है, हमें तुम्हारी क्या पहचान?” आरोव ने दस्तावेज़ दिखाए—कुछ फंड का प्रस्ताव, बाहरी दानदाताओं की सूची, शहर में बने कुछ NGO के पत्र। पटेल जी ने चढ़कर चाय पी, थाली में पकौड़े रखवाए, पर तब तक गाँव वालों की नकारात्मक ऊँची-नीची बातें चाय की तासीर से भी गहरी थी। “ये शहरों का खाना है, यह लड़का बदल गया है,” और “जो यहाँ का नहीं, यहाँ क्या जाने?”—ऐसे अनगिनत स्वर आहत कर रहे थे।
मगर कविता की मासूम मुस्कान अप्रतिहत रही। वह रोज़ स्कूल की कच्ची कक्षाओं में झाँककर आँखे चमकाए खड़ी रहती। बच्चों को दिखाती—“देखो ये खिड़कियाँ, ये दरवाज़े, ये दीवारें—एक दिन तुम इन्हें रंग भरो और इनमें हँसी भर दो।” एक दिन उसने गाँव के औरतों को इकट्ठा किया, खाते-पीते चेहरे थे, कुछ दुपट्टे का किनारा चाट रही थीं। कविता बोली, “माँए, आप फिर से सिलाई कर लिया करो, मैं खुद पर व्यायाम करके स्कूल के पर्दे सिलवाऊँगी, और आप जन-जन तक नयी यूनिफ़ॉर्म पहुँचाना।” सबने उसे हलकी-सी हँसी में उड़ा दिया, पर बाद में देखा—वह बुज़ुर्ग छत पर छापी मशीन खोजने गई थी, और अगली सुबह गाँव में कोई मुफ्त सिलाई का अनाउंसमेंट मिला।
फिर आया ठेका ठोकर का पल। गाँव के ज़मींदार, थॉकर सिंह, ने कहा, “तुम कैसे स्कूल खोलने का काम करोगे? यह फिल्ड मुझारा मिले हुए जमीन है, मैं सार्वजनिक भूखण्ड पर काम नहीं होने दूँगा।” पटेल जी का वजन कुछ कम हो गया, कुछ शब्द भीतर दब गए। मगर उस समय आया एक चिट्ठी का जवाब—एक बड़े शहर से आया बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मैन्युअल। लिखा था कि ग्राम स्तर पर शिक्षा परियोजनाओं के लिए अनुदान मिले हैं। ये पत्र थॉकर सिंह के हाथ तक पहुंचा, और उसने खुद उस फ़ाइल को खोला। उसमें दस लाख रूपये तक का बजट था, किताब, मेज़- कुर्सी खरीदने के लिए, और शिक्षकों को मानदेय देने के लिए। वह पल उसका चेहरा बदल गया, जैसे सूखे खेतों में अचानक बारिश हो गई हो।
आरोव ने थॉकर सिंह को धन्यवाद दिया और उनके आदेशानुसार स्कूल की मरम्मत शुरू हुई। मिट्टी की दीवारें गिराई गईं, ईंटों की दीवारें खड़ी की गईं, प्लास्टर करवाया गया, नई खिड़कियाँ लगा दी गईं, बिजली के तार बिछाए गए, पक्के फर्श पर रंग चढ़ा, और एक दिन स्कूल का प्रधानाध्यापक आया—नरेश सर, जिन्होंने उस फंड को गिरवी न रखकर सही उपयोग किया, देखकर ताली बजाई। पहले दिन स्कूल में सिर्फ दस विद्यार्थी आए थे, मगर दसवें दिन हॉल भर गया। कविता भी रोज़ सबसे आगे खड़ी होती, सीट भी पक्की थी, ब्लैकबोर्ड भी खरा, और सर की अब आवाज़ में वह गंभीरता थी, जिसने गाँव की पुरानी उदासीनता को जगा दिया।
समय के साथ गाँव बदलने लगा। खेतों में नालियाँ साफ़ होने लगीं, पानी निकासी बेहतर हुई, गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा, ख़ासकर लड़कियाँ अब घरों से निकलकर स्कूल आतीं। कविता की माँ, सुमित्रा, ने भी सिलाई सिखाने का केन्द्र खोला, और पूरे आँचल में महिलाएँ पहुँचने लगीं। गाँव के बुज़ुर्ग चकित थे—पहले जो चुप रहने वाले थे, अब खुलकर बोलते, स्कूल की फ़ंडिंग का हिसाब-किताब माँगते, नए प्रोजेक्ट्स की सूची बनाते। पटेल जी ने गाँव में पंचायत के प्रथम पायदान पर ताली बजा कर घोषणा की कि इस स्कूल की सफलता ने ‘पावनपुर मॉडल’ स्थापित कर दिया, और आसपास के तीन गाँव भी इसी तरह की पहल करेंगे।

इसी बीच शहर में समाचार पत्रों ने भी ‘पावनपुर की सुबह’ नाम से फीचर छापा। आलेख में लिखा था—‘एक उद्यमी ने अपने दादा के सपने को पूरा किया, एक मासूम ने विश्वास का दिया जलाया, और पूरा गाँव उजियारा बन गया।’ उस खबर के लिंक को कट-पेस्ट करके बिखरे हुए गाँव की लाइब्रेरी में सजा दिया गया। एक छोटा कंप्यूटर रूम भी बना, जहाँ दूर-दराज के बच्चे इंटरनेट की दुनिया से जुड़ते हुई तस्वीरें देखते, रिमोट-लीARNING करते। कविता स्वयं IT ट्रेनिंग ले रही थी, और आशा थी कि एक दिन वह “डिजिटल गाँव” का मिसाल बने।
अगले वर्ष जब गांव में पहली बार वार्षिक विज्ञान मेला लगा, तो कविता ने ‘सौर ऊर्जा चार्जर’ का मॉडल दिखाया, जिससे स्कूल के बल्ब और मोबाइल चार्ज हो जाते थे। थॉकर सिंह के खेत पर लगे सोलर पैनल्स ने उसकी ‘प्रोजेक्ट’ को असल धरातल पर उगाया। आरोव ने उत्सव के मंच से कहा, “यह मॉडल सिर्फ ऊर्जा नहीं, उम्मीद का मॉडल है। इसने हमें दिखाया कि छोटे कदमों से बड़े बदलाव आते हैं।” उस दिन सबने तालियाँ बजाईं। कविता की आँखों में गर्व था, सुमित्रा की आँखों में आँसू, और आरोव की उंगलियाँ ब्लॉग पर लाइव अपलोड कर रही थीं—कि कैसे मिलकर एक दादा के सपने को पूरा किया गया, एक मासूम की हिम्मत से पूरे गाँव को शिक्षित किया गया।
समय का पहिया और घूमता गया। पाँच साल बाद जब आरोव फिर से शहर लौटने की तैयारी करने लगा, तब गाँव का विकास चरम पर था—प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल चुका था, दूरस्थ शिक्षा कक्षाएँ चल रही थीं, और गली-गलियारे हर सुबह गीत-सी ख़ुशी बिखेरते थे। पटेल जी ने भावुक होकर हाथ जोड़ा, “बेटा, तूने गाँव को नई आस दी है। तेरे बाद अब कई लोग आएंगे, और यह काम आगे बढ़ेगा।” कविता ने जरा लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, “भैया, आप जाओ—हम संभाल लेंगे।” आरोव को आँसू रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने आँखों से कहा, “तुम्हारी मुस्कान मेरी धड़कन है, याद रखना।”
शाम को स्टेशन पर चाय की दुकान के पास सारा गाँव इकठ्ठा था। पटरी पर खड़े होकर उन्होंने गीत गाया, ताली बजाई, और कविता ने अपने हाथों से बनाए गुड़ के लड्डू बाँटे। ट्रेन की सीटी बजी, जैसे किसी नए दौर की शुरुआत हो। आरोव खिड़की से बाहर झाँका, चेहरे पर मुस्कान, आँखों में आंसू, और गाँव की मिट्टी ने इतने प्यार से गले लगाया कि उसकी साँसों में तीव्रता आ गई। वह जानता था—वह चाहे कितनी दूर चला जाए, पावनपुर का उजियारा हमेशा उसके साथ रहेगा।
ट्रेन निकल गई, धुंध का धब्बा पीछे छूट गया, और सूरज की किरणों ने गाँव की कच्ची सड़कें फिर से सुनहरी कर दिया। उस सुनहरी मिट्टी में अब कोई टूटी पाठशाला नहीं, कोई सूनी पंचायत भवन नहीं, बल्कि सब कुछ नए सिरे से जीवंत था। गाँव के बच्चे पढ़ते, खेलते, खिलखिलाते, और कविता अपनी आईटी लैब में उभरती तकनीकियां सीखते। वही कविता, जिसने कभी टूटी घंटियाँ ढूँढ़ी थीं, अब अनगिनत घंटियाँ बजने का कारण बनी थी।
और इस तरह एक नौजवान की उनकी दादा की यादों से जन्मी चाहत, एक मासूम लड़की के विश्वास की चमक, और पूरे गाँव के प्रयास की एकता ने मिलकर पावनपुर को उजाले का गाँव बना दिया। यह कहानी याद दिलाती है कि सपनों की जड़ें कभी छोटी नहीं होतीं; जब हमें विश्वास और साहस साथ हो, तो धुंध में भी कोई राह दिख जाती है, टूटी दीवारों में भी हँसी खिल उठती है, और गाँव-शहर, इंसान-इंसानियत की दूरी मिट जाती है। अपने भीतर उस दीये को कभी बुझने मत देना—क्योंकि एक दीया जला कर ही दस-दस दीयों को रोशन किया जा सकता है।
News
“जब लालच ने ली इंसानियत की परीक्षा | बुज़ुर्ग पिता, बहू और IPS बेटी की सच्ची कहानी”
“जब लालच ने ली इंसानियत की परीक्षा | बुज़ुर्ग पिता, बहू और IPS बेटी की सच्ची कहानी” . . धर्मपाल…
10 साल का अनाथ बच्चा एक करोड़पति की कार साफ करता था || उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा
10 साल का अनाथ बच्चा एक करोड़पति की कार साफ करता था || उसे नहीं पता था कि आगे क्या…
फटे कुर्ते वाला बुज़ुर्ग जब बैंक गया तो सब हंसे… लेकिन कुछ घंटे बाद सबकी हंसी गायब!
फटे कुर्ते वाला बुज़ुर्ग जब बैंक गया तो सब हंसे… लेकिन कुछ घंटे बाद सबकी हंसी गायब! . . सुबह…
अपंग पिता ने 13 साल की गर्भवती बेटी की परवरिश की – बच्चे के पिता की पहचान जानकर पूरा गाँव हिल गया।
अपंग पिता ने 13 साल की गर्भवती बेटी की परवरिश की – बच्चे के पिता की पहचान जानकर पूरा गाँव…
पति रोज़ चुपचाप अपमान सहता रहा, बस इसलिए कि घर टूटे नहीं… फिर जो हुआ, किसी ने सोचा नहीं था
पति रोज़ चुपचाप अपमान सहता रहा, बस इसलिए कि घर टूटे नहीं… फिर जो हुआ, किसी ने सोचा नहीं था…
करोड़पति लड़की बोली – तेरे जैसे लड़के मेरे जूतों के नीचे होते हैं !
करोड़पति लड़की बोली – तेरे जैसे लड़के मेरे जूतों के नीचे होते हैं ! . . सूरज की पहली किरणें…
End of content
No more pages to load