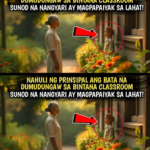जिस बेटे को डॉक्टर 9 साल से ढूंढ रहा था- वो सड़क पर समोसे बेचता मिला फिर…

दिल्ली का सर्द मौसम। धुंध में डूबी सड़कों पर वाहनों की हेडलाइटें किसी खोए हुए कारवां की मशालों की तरह झिलमिलाती थीं। आनंद विहार बस अड्डे के बाहर, धूल भरी पटरी पर एक छोटा-सा ठेला रोज तड़के से आकर खड़ा हो जाता था। ठेले के ऊपर एक पुरानी, पर साफ-धुली नीली चादर, स्टील के दो डब्बे—हरी और लाल चटनी के, और एक बड़ा-सा कड़ाहा, जिसमें तेल की सतह पर प्रतिबिंबित होती सुबह की पहली धूप किसी सुनहरी उम्मीद का भ्रम देती थी। उस ठेले का मालिक—बारह बरस का पतला-दुबला, पर तेज़ नजरों वाला लड़का—राहुल।
राहुल सुबह चार बजे उठता। कंबल की झुर्री झटककर वह उस छोटी-सी झोपड़ी के बाहर आता जिसे वह “घर” कहता था। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर फफूंद के धब्बे थे, हवा में दवा और धुएं की मिली-जुली गंध। अंदर, पुरानी चारपाई पर शारदा अम्मा खांसती हुई करवट बदलतीं। उनकी उम्र साठ के करीब थी, पर गरीबी और काम के बोझ ने उन्हें कहीं बुज़ुर्ग बना दिया था। सफेद सूती साड़ी, माथे पर हल्की-सी बिंदी, और आँखें—जैसा कि जिंदगी की धूल के नीचे छिपा कोई झरना।
“अम्मा, दवा का टाइम हो गया,” राहुल फुसफुसाकर कहता।
शारदा अम्मा मंद मुस्कान देतीं—“पहले तुम चाय पी लो, बेटा।” वह आवाज़ जो किसी मंदिर की शांति जैसी शीतल होती, पर भीतर बीमारी की चीख़ दबाए रखती।
राहुल पहले चूल्हे पर पानी चढ़ाता, चाय बनाता, फ़िर कड़ाही में तेल डाल देता। आलू उबलते, मसाले भूनते, आटा गूँधता। उसके छोटे-छोटे हाथ किसी अनुभवी हलवाई की तरह तेज़ी और सावधानी से काम करते। सूरज निकलने से पहले वह ठेला धकेलते हुए बस अड्डे तक पहुँच जाता।
ठेले के आगे दो पुरानी लकड़ी की बेंचें रखी थीं—झुकी हुई, थोड़ी काँपती हुई—पर हर दिन कुछ नए लोग उन पर बैठकर गरम-गरम समोसों का स्वाद लेते। राहुल के समोसे तीन तरह के। मसालेदार आलू, तीखे प्याज, और मिक्स—जिसमें थोड़ा-सा मटर, थोड़ी-सी मूँग, और थोड़ी-सी रचनात्मकता। लोग खाते तो उंगलियाँ चाटते। “छोकरे, चटनी बढ़िया है,” कोई कहता। “बाप रे, झुर्र-झुर्र कर रहा है अंदर,” कोई हँसता। राहुल झेंपकर मुस्कुरा देता।
पर हर दिन की तरह, तनाव की एक छाया भी उसके दिन के ऊपर तैरती रहती—सफेद जीप की छाया। दस बजे के आसपास सड़क की धूल पर उस जीप के टायरों का निशान उतरता और राहुल का दिल धक-धक करने लगता। जीप से उतरते छह चेहरे—रुखे, भारी आवाज़ वाले, वर्दी की अकड़ और आँखों में आदेश। सबसे आगे—राजेश सिंह। उसके पीछे विनोद मिश्रा, अशोक यादव, प्रदीप गुप्ता, नरेश चौहान, और कमलेश पांडे। स्थानीय थाने के सिपाही—जो कानून का डर फैलाने के लिए थे, पर यहाँ—वे राहुल के ठेले पर मुफ्त का भोजन लेने आते।
“अरे राहुल छोकरे!” राजेश सिंह की भारी आवाज़। “छह प्लेट पटक दे… और सुन, आज तीखी चटनी ज्यादा डालना।”
राहुल की उंगलियाँ तेज़ी से चलतीं। प्लेटें सजतीं, चटनी बिखरती, पानी का जग इधर-उधर। वे खाते, ठहाके लगाते, किसी कवि की कविता पर हँसी उड़ाते, किसी गरीब की दुर्दशा पर मज़ाक। खाना खत्म होता और वे उठ जाते—जैसे वे कोई मेहरबानी करके जा रहे हों। राहुल धीमे से कहता—“साहब, आज… अम्मा की दवा—”
“क्या कहा?” राजेश सिंह की भौंहें तनतीं।
“₹80… साहब,” राहुल की आवाज़ और भी धीमी।
“हमसे पैसे मांगेगा?” विनोद मिश्रा हँसता—“ओए, समझा इसे। हम यहाँ खाते हैं तो इसकी दुकान की शान बढ़ती है।”
सड़कों पर चलते लोग देखते। कोई दो पल ठहरता, फिर चल देता। किसी को अपनी बस पकड़नी होती, किसी को अपनी नौकरी, किसी को अपनी नैतिकता। हर दिन यह होता और हर दिन राहुल एक नया घूँट निगल जाता—अपनी गरिमा का, अपने आत्मसम्मान का।
सर्दी की एक सुबह, धूप बस उतरने ही वाली थी कि शारदा अम्मा अचानक बेहोश हो गई। उनकी साँस घरघराने लगी। राहुल ने उधड़ी-सी चप्पल पहनी, अम्मा को कंबल में लपेटा, एक रिक्शेवाले से हाथ जोड़कर कहा—“भैया, अस्पताल…” सरकारी अस्पताल की दीवारों पर दवा कंपनियों के पोस्टर्स, गलियों में कतारें, और डॉक्टर की निष्प्रभावी आवाज़—“फेफड़ों में संक्रमण है। दवाइयाँ महँगी हैं। कम से कम पच्चीस हजार।”
राहुल ने अपनी जेब टटोली—तीन हजार। महीनों की बूँद-बूँद। डॉक्टर की कड़क नज़र—“दवा चाहिए तो पैसा चाहिए, बेटे।”
अगले दिन से एक और दौड़ शुरू हुई। चार बजे उठना, समोसे की थाली बढ़ाना, और ज्यादा तेजी से बेचना। अब उसकी उंगलियाँ और भी फुर्तीली हो गईं—क्योंकि जरुरत की रफ्तार तेज़ थी। पर वे जीप और वे लोग—अब और भी बेझिझक। एक दिन आठ, अगले दिन दस, फिर पंद्रह। हर रोज़ वे आते, खाते, और हँसते हुए चले जाते। राहुल की कमाई का आधा—कभी उससे भी ज्यादा—अँधेरे में समा जाता।
एक महीने में वह आठ हजार जोड़ पाया। अम्मा की हालत गिरती जा रही थी। रात को वे खाँसतीं—राहुल कंबल में उनका सिर सहलाता। “बेटा,” उनकी आवाज़ कहीं दूर से आती—“मैं कहीं मर तो नहीं जाऊँगी।” राहुल का दिल चीरता, पर वह मुस्कुरा देता—“अम्मा, चुप। मैं हूँ न।”
एक दिन, जब वे छहों हँसते-हँसते प्लेटें छोड़े उठने लगे, राहुल ने हिम्मत करके कहा—“साहब, प्लीज… मेरे पैसे दे दीजिए। अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। दवा—”
वाक्य पूरा नहीं हुआ। राजेश सिंह का चेहरा तमक उठा। “अबे साले!” उसने अचानक ठेले पर लात मारी। ठेला चरमराया, लुढ़का, और समोसे—वे गरम-गरम, मेहनत की भूनी हुई गाँठें—सड़क पर बिखर गए। कड़ाही का तेल छलककर राहुल के हाथ और पैर पर गिरा। वह चीखा—“आह!” पर चीख कानों तक नहीं पहुँची। विनोद ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा—“आइंदा पैसे मांगे तो ठेला जप्त।” प्रदीप ने समोसों को लात से उछाला, नरेश ने धक्का देकर उसे गिराया, कमलेश ने सिर पर वार किया। लोग भीड़ बनकर खड़े थे—चुप्पियों की भीड़। एक बच्चे पर छह वर्दियों का जुल्म; एक शहर की आत्मा का मौन।
वे चले गए, अपनी जीप में बैठकर, प्रदूषण में खोते हुए। राहुल फुटपाथ पर बैठकर रोता रहा। कुत्ते बिखरे समोसों को खाते रहे—जैसे गरीबी पर प्रकृति की अंगुली।
उसी भीड़ में, बिजली विभाग का एक लाइनमैन खड़ा था—पंकज। सादी-सी शर्ट, कंधे पर औज़ारों का थैला, आँखों में सच्चाई की रेखाएँ। वह थाने की खराब लाइन ठीक करने निकला था। उसने देखा—सब देखा। बचपन से उसने अपने पिता को ईमान का अर्थ सिखाते हुए देखा था। उसका एक बेटा था—राहुल की उम्र का। उसने एक पल को सोचा—अगर यह मेरा बेटा होता? उसके भीतर आग-सी भड़की। उसने जेब से मोबाइल निकाला—वीडियो चालू। फ्रेम में सब कुछ था—ठेला गिरते हुए, कड़ाही का तेल गिरते हुए, थप्पड़ की आवाज़, बच्चे का रोना। पंकज के हाथ काँपे नहीं। उसने उस अमानवीयता को कैद कर लिया जो अक्सर हवा में घुलकर अदृश्य हो जाती है।
थाने पहुँचा तो हॉल की बत्ती खराब थी। उसके दिमाग में एक योजना चमकी। वह वायरिंग के पास झुका, निरीक्षण का नाटक किया, और फिर—मुख्य स्विच बोर्ड के तारें उसने इस तरह “जोगाड़” कर दीं कि जब तक वह चाहें, तब तक मुख्य हॉल अंधेरे में डूबा रहे। फ्यूज़ निकाल लिया, तारों का क्रम बदल दिया, कनेक्शन की ऐसी चाल बनाई कि दीवारें मौन रहें।
एक घंटे बाद, राजेश सिंह और साथी लौटे। थाने का मुख्य हॉल अंधेरे में डूबा हुआ। “अरे पंकज!” राजेश सिंह की झल्लाती आवाज़—“क्या खिचड़ी पक रही है? बत्ती क्यों नहीं आई?”
पंकज, शांत, पर आँखों में बिजली—“पहले सवाल मैं करूँगा, साहब। उस समोसे वाले बच्चे के पैसे क्यों नहीं दिए आपने?”
कमरा सन्न। उसकी बात हवा को चीर गई। विनोद चीखा—“अरे, यह बोल क्या रहा है! लाइनमैन है या नेता? अपना काम कर, समझा?”
पंकज ने मोबाइल निकाला—“वीडियो मेरे पास है। सब कुछ।” उसने स्क्रीन पर चलती झलकें उन्हें दिखा दीं। राजेश सिंह का चेहरा घोर का, फिर फीका। अशोक ने दाँत भींचे—“वीडियो डिलीट कर दे, वरना…”
पंकज की आवाज़ पहली बार कँपी—डर से नहीं, अपने ही संकल्प का बोझ उठाते हुए—“नहीं करूँगा। जब तक आप उस बच्चे को पैसे नहीं देंगे। जब तक आप माफी नहीं माँगेंगे। जब तक आप… इंसान नहीं बनेंगे।”
हिंसा की आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया। थाप्पड़—लात—घूँसा। कपड़े फटने की आवाज़। पंकज एक दीवार से टकराया, फिर भी मोबाइल को छाती से चिपटाए रखा। “मैं न्याय की बात कर रहा हूँ,” उसने कहा। “आप गलत—”
“बहुत बोलता है,” प्रदीप ने धक्का दिया। पर एक क्षण में, शायद उनकी समझ में आया कि यह आग यदि बाहर निकली तो वे जलेंगे। या शायद उन्हें भरोसा था कि हत्या करके निकल भी जाएँगे। जो भी हो—वह क्षण बीत गया। वे उसे छोड़कर हट गए। पंकज लड़खड़ाता हुआ बाहर आया—रक्त की पतली धारा उसकी भौंह के पास। वह सीधे अपने घर नहीं गया। उसने अपने पुराने दोस्त, स्थानीय टीवी रिपोर्टर—राज—को फोन किया।
“राज, एक वीडियो है। तू इसे देख और बोल कि यह देश किस ओर जा रहा है।”
राज ने देखा। उसने अपनी आँखें मल लीं—जैसे स्क्रीन कोई ख्वाब दिखा रही हो। “यह रात की खबर नहीं, यह देश की खबर है, पंकज।” चैनल के मालिक के पास वह सीधे पहुँचा। शाम सात बजे—प्राइम टाइम। हेडलाइन—“बारह साल के बच्चे पर दिल्ली पुलिस का कहर।” वीडियो चल पड़ा। घरों में बैठे लोग टीवी की तरफ झुक गए। राहुल रो रहा था—और शायद पहली बार, शहर की आत्मा को अपनी ही आवाज़ सुनाई दी।
सोशल मीडिया पर वीडियो ज्वाला की तरह फैला। “#न्याय_राहुल_के_लिए” ट्रेंड करने लगा। कॉलेजों के छात्र, दफ्तरों के कर्मचारी, घरों की महिलाएँ—सबने शेयर किया। लोग बोले—देखो, कानून के रक्षक कैसे बन गए हैं भक्षक। मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर पर दबाव बढ़ा। चैनल वालों ने थाने की छवि धुँधली होते दिखलाई—जैसे अंधेरे में खड़े हों अधिकारी, उजाले में खड़ा हो एक बच्चा।
अगले तीन दिनों में मीडिया आनंद विहार की झोपड़ी तक पहुँच आयी। कैमरे, माइक्स, बूम रोड—तारों का इकट्ठ। रिपोर्टर ने राहुल से पूछा—“बेटा, क्यों मारा उन्होंने?”
राहुल की आवाज़ अभी भी काँपती—“साहब, मैंने अपने पैसे माँगे थे… अम्मा बहुत बीमार हैं।”
“अम्मा कौन?”—रिपोर्टर ने शारदा की तरफ देखा।
शारदा अम्मा का चेहरा कैमरे के सामने आया। “यह मेरा अपना बेटा नहीं है,” उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ में समय की धूल उड़ती हुई—“नौ साल पहले, यमुना में बहता हुआ मिला था। मैंने इसे उठाया, अस्पताल ले गई, पुलिस में खबर दी… कोई नहीं आया। मैंने इसे अपने साथ रख लिया। इसका नाम रखा—राहुल। और तब से…”
एक और खिड़की खुली। अब यह सिर्फ़ एक पुलिस बर्बरता का मामला न रहा। यह एक खोए हुए बच्चे की कहानी भी बन गया। “#राहुल_का_घर_ढूँढो”—नया हैशटैग। लोग अपनी-अपनी कल्पनाएँ और संदेह जोड़ते। पुरानी खोई हुई बच्चों की खबरों के साथ उसे जोड़ते।
शहर के दूसरी तरफ, एक आधुनिक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में, डॉ. अनिल वर्मा पाँच घंटे से एक बच्चे का हार्ट ऑपरेशन कर रहे थे। दिल्ली के सबसे नामी हृदय सर्जन, जिनके संकेत पर दर्जनों हाथ काम करते, जिनकी शब्दहीन आँखों का इशारा जीवित और मृत के बीच पुल बन जाता। ऑपरेशन पूरा हुआ। उन्होंने मास्क उतारा। पसीने की बूँदें उनके माथे से फिसलीं। फोन उठाया—सैंकड़ों मिस्ड कॉल्स। पत्नी प्रिया का मैसेज सबसे ऊपर—“अनिल, टीवी देखो—कहीं वह हमारा अर्जुन तो नहीं? नौ साल पहले…” उनकी उँगलियाँ काँप गईं। टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर राहुल—कपड़ों का रंग फीका, आँखों का रंग गहरा। अनिल की साँस अटक गई। चेहरे का नाक-नक्श, होंठों की बनावट—यादों की किताब खुली। कैलांगुट बीच। मई का सूरज। लहरें। तीन साल का अर्जुन। शंख से खेलता, फिर किसी लहर में खोता हुआ। सालों की तलाश। अख़बारों में इश्तहार। निजी जासूस। समंदर की अनंतताओं में झाँकती हुई आँखे। एक दिन सच ने हार मान ली—या उम्मीद थक गई। पर आज—टीवी पर—क्या यह उसी उम्मीद का पुनर्जागरण है?
उन्होंने अपने वकील मित्र राकेश शर्मा को फोन किया—“तुरंत आनंद विहार जाओ। डीएनए टेस्ट। मैं शक कर रहा हूँ—वह अर्जुन है।” पुलिस मित्र इंस्पेक्टर रमेश को भी लगाया—“साथ जाना।”
शाम ढल रही थी, जब राकेश और रमेश झोपड़ी पहुँचे। कैमरों की भीड़। राहुल शारदा अम्मा के पास बैठा, उनकी दवा का टाइम देखता हुआ। राकेश ने शारदा को सब समझाया—“एक डॉक्टर का बेटा नौ साल पहले खो गया था। शक है… डीएनए टेस्ट कराना होगा। अम्मा, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपने जो किया है—उसका कोई ऋण चुका नहीं सकता। चाहे रिपोर्ट क्या आए—आप उसकी माँ हैं… यह सच नहीं बदलता।”
शारदा की आँखों में पानी भर आया—डर और विश्वास के बीच तैरते आँसू। “बेटा,” उन्होंने राहुल का सिर थपथपाया—“जो भी होगा, हम साथ रहेंगे।” राहुल ने घबराकर कहा—“मैं अम्मा को छोड़कर नहीं जाऊँगा।” राकेश ने मुस्कुराकर कहा—“किसने कहा जाने को? सच का पता लगाना बुरा नहीं।”
डीएनए सैंपल लिए गए। एक रात—लंबी—घड़ी की सुइयों ने जैसे हर सेकंड में एक-एक वर्ष डाल दिया। सुबह दस बजकर तीस मिनट। राकेश का फोन—“अनिल… सौ प्रतिशत मैच।” शब्द हवा में तैरते हैं, कभी-कभी पत्थर बन जाते हैं। फोन अनिल के हाथ से फिसल गया। नौ साल का घाव एक पल में भर नहीं जाता—पर उसी पल से भरना शुरू हो जाता है।
अस्पताल का लंबे गलियारा, कार के टायरों की आवाज़, कैमरों की भीड़, और फिर—झोपड़ी के बाहर एक चमकता हुआ सन्नाटा। डॉ. अनिल वर्मा और प्रिया, हाथों में समय की थरथराती रेखाएँ लिए, उस कमरे के सामने खड़े जिसमें उनकी दुनिया वापस मिलने वाली थी। प्रिया की आँखों में आँसू—वे आँसू जो सालों से अंदर रुके हुए थे। वे अंदर आईं। राहुल ने सिर उठाया। चेहरे पर एक अनपहचानी पहचान की हल्की सी मुस्कान दौड़ी। अनिल आगे बढ़े—धीमी चाल, कंपन भरे हाथ, और फिर एक अनन्त आलिंगन—जिसमें खोए वर्ष भी समा जाएँ, जिसमें समुद्र की खारापन भी मीठा हो जाए। प्रिया ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर देखा—“अर्जुन…”
“मुझे राहुल बुलाइए,” उसने धीरे से कहा—“यह नाम अम्मा ने दिया है।” कमरे में एक मौन सहमति का आलोक फैला। अनिल ने शारदा के पैर छुए—“अम्मा… आपने हमारा बच्चा बचाया। नौ साल… शब्द छोटे पड़ जाते हैं।”
उसी दिन, अनिल ने शारदा अम्मा को अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। श्रेष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट, एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइज़र, पोषण—सब कुछ। राहुल अस्पताल के कमरे में उनके सिरहाने बैठकर वही करता रहा जो वह हमेशा करता था—समय देखता, दवा देता, मुस्कुराता, हिम्मत देता।
पर कहानी का वह हिस्सा जिसमें जुल्म की धूल थी—वह वहीं नहीं छोड़ी जा सकती थी। अनिल ने राकेश से कहा—“अब कानून बोलेगा। उन छहों पर सख्त धाराएँ लगाओ—बाल अधिकार हनन, दादागिरी, शारीरिक हिंसा, भ्रष्टाचार…” इंस्पेक्टर रमेश ने खुद को इस केस से अलग रखा—हितों के टकराव से बचने के लिए—पर उसने यह सुनिश्चित किया कि जाँच निष्पक्ष हो। राजेश सिंह, विनोद, अशोक, प्रदीप, नरेश और कमलेश—छहों गिरफ्तार।
मीडिया के कैमरों ने इस बार अदालत के बाहर चौकियाँ संभाल लीं। कोर्ट रूम के अंदर, न्यायाधीश की तीखी नजरों से कपट की परतें छिलती गईं। सबूत—पंकज का वीडियो—अडिग। गवाह—शारदा अम्मा—सच की आँखें। डॉक्टर अनिल—प्रभावित पक्ष—पर उनके शब्द संयमी। पंकज को कोर्ट ने सराहा—“यह नागरिक साहस है, जिसके सहारे लोकतंत्र सांस लेता है।”
दो महीने—तेज़। शायद इसलिए कि शहर जाग चुका था। जज ने फैसला सुनाया—“छहों दोषी। दो-दो वर्ष की सजा। पचास-पचास हजार का जुर्माना। नौकरी से बर्खास्तगी।” शासन का आदेश—“विभागीय जाँच पूरी होने तक निलंबन”—अब औपचारिकता बन चुका था। थाने के बाहर कुछ लोगों ने ताली बजाई—कुछ ने कहा—“कम है।” पर न्याय की यात्रा में पहला पड़ाव भी महत्वपूर्ण होता है।
शारदा अम्मा के फेफड़े धीरे-धीरे साफ होने लगे। नेबुलाइज़र की धुंध में अब एक युवा जीवन का प्रकाश घुलने लगा। अनिल अस्पताल के कमरे में उनके पैरों के पास बैठते—“अम्मा, आप हमारे साथ रहिए।” शारदा हँसतीं—“तुम डॉक्टर हो, बात जैसे दवा। पर मेरा घर?”— Friendliness में छिपी चिंता। “अम्मा,” प्रिया ने उनकी हथेलियाँ थामीं—“घर आपका है, बेटा आपका है। बस घर बड़ा हो जाएगा।”
अस्पताल से छुट्टी मिली। शहर के किसी पॉश इलाके में एक सफेद बंगला—अंदर बोगनविलिया की शाखें, उस पर लगे गुलाबी फूल। ग्रिल के पास एक छोटा सा स्विंग। वॉलपेपर पर नीले सितारे। प्रिया ने कुछ ही दिनों में एक कमरा ऐसा बना दिया जिसमें राहुल अपने पुराने दिनों की कोई याद न ढूँढ सके—पर अपनी पहचान न खोए। दीवार पर एक फ्रेम—“राहुल/अर्जुन।” दोनों नाम। दोनों सच।
राहुल पहले दिन उस कमरे में चुपचाप बैठा रहा। बड़े बिस्तर की चादर छूकर देखा। मेज़ पर रखी किताबें खंगालीं—अक्षर उसके सामने नाचने लगे। “मैं पढ़ना चाहता हूँ,” उसने धीरे से कहा। अनिल की आँखें चमकीं—“और हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो। जितना पढ़ना चाहो। पर एक बात—तुम्हारा ठेला, तुम्हारी चाय, तुम्हारे समोसे… तुम चाहो तो कभी-कभी हमारे यहाँ भी बनाओ। हम सब मिलकर खाएँगे।” उस घर में पहली बार हँसी ऐसी गूँजी जैसे बारिश के बाद पहली धूप।
कुछ हफ्ते बीते। राहुल एक अच्छे स्कूल में दाखिल हुआ। उसकी उम्र के बच्चों ने उसे देखा—कुछ ने धीरे से फुसफुसाया—“यही है न वो टीवी वाला?” राहुल ने एक पल को सिर झुका लिया—फिर याद आया, अम्मा ने कहा था—“नाम से नहीं, काम से शरीफ बनते हैं।” वह मुस्कुरा दिया।
स्कूल की लाइब्रेरी में उसने पहली बार डिकेन्स की कहानी पढ़ी—ओलिवर ट्विस्ट। वह हँसा और रोया—“यह तो मेरी तरह…” उसने महसूस किया कि कहानियाँ सिर्फ दूसरों की नहीं होतीं—वे हमारी भी होती हैं। उसने संगीत कक्ष में ढोलक उठाई, ताल बद्ध करना सीखा। एक दिन कविता पाठ में उसने मंच पर खड़े होकर बोला—“नाम देता है समाज, पर पहचान बनाते हैं हमारे कर्म।” तालियाँ बजीं—और तालियों के पीछे कोई रुदन नहीं था, कोई जुल्म नहीं था—सिर्फ़ स्वीकार।
शारदा अम्मा अब बंगले के पिछवाड़े की धूप में बैठतीं। पोर्टेबल नेबुलाइज़र अब कभी-कभार। उनकी हथेलियाँ हमेशा व्यस्त—राहुल के लिए ऊनी टोपी बुनतीं, प्रिया के लिए किचन में “चना-जोर” बनातीं। नाम से वे “अम्मा” ही रहीं—राहुल के लिए और धीरे-धीरे अनिल और प्रिया के लिए भी। उनके कमरे में एक फोटो फ्रेम—झोपड़ी वाले दिनों की एक धुंधली तस्वीर—जिसमें राहुल मुस्कुरा रहा है, गालों पर धूल, आँखों में उजाला। और फ्रेम के पास, एक नया फोटो—सभी एक साथ, एक बगीचे में। समय ने खुद अपने दो चित्र एक साथ टाँग दिए थे।
पर कहानी का एक धागा अभी बाकी था—पंकज। पंकज ने अपना काम करना जारी रखा। अपनी चोटों पर मरहम, अपने मोबाइल में वीडियो। एक दिन अस्पताल में आयोजित एक छोटे से समारोह में उसे सम्मानित किया गया—“बाल अधिकार रक्षक”—एक छोटे शहर-सा खिताब। मंच पर अनिल ने कहा—“अगर पंकज जैसे लोग हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा शहर सिर्फ इमारतें नहीं, इंसान भी बना रहा है।” तालियाँ बजीं। पंकज ने सिर झुकाया—“मैंने जो किया, वह हर पिता करता।” उसकी आँखें भर आईं—“मेरा बेटा कहता है—पापा, आप हीरो हो।” यह शायद सबसे बड़ा पुरस्कार था।
राहुल ने एक दिन पंकज के घर जाने की जिद की। दो कमरे का घर, दीवार पर देवी-देवताओं के कैलेंडर, कोने में तारों का मोड़ा हुआ गठ्ठर। पंकज की पत्नी ने चाय बनाई। पंकज का बेटा—रवि—झेंपता हुआ आस-पास। राहुल और रवि बाहर निकलकर खेल में लग गए—कंचे, गिल्ली-डंडा, फिर एक पुरानी टूटी साइकिल। उन्होंने हँसी को फिर से गली में लौटते देखा। पंकज की पत्नी ने शरदा अम्मा के पैर छुए—“ताईजी, आप ने जिसे पाला…” शारदा ने हँसकर कहा—“जिसे हमने पाला, अब पूरी दुनिया पूछती है। पर यह दुनिया तभी दुनिया बनेगी जब वह पालेगी—न कि सिर्फ़ देखेगी।”
समय की नदी फिर देश की व्यस्त सड़कों की तरह बहती रही। एक साल बीता। राहुल का चेहरा भरा-भरा हो गया—स्वस्थता की चमक। उसने वायलिन सीखना शुरू किया। उँगलियाँ, जो कभी आटा गूँधती थीं, अब तारों पर फिसलतीं। वह अपने गाने लिखता—“समोसा और सितारे”—एक ओड टू अम्मा, एक ओड टू कड़ाही, एक ओड टू स्विंग। वह थियेटर ग्रुप से भी जुड़ा—सड़क नाटक—“कानून की छाया”—जिसमें वह उस दिन का दृश्य मेकअप के साथ खेलकर दिखाता—पर अंत में, वह एक लाइन बोलता—“जुल्म हमेशा हारता है, मगर हार उस दिन से शुरू होती है जब कोई एक आदमी ‘न’ कहता है।”
और शहर? शहर भूलता है—या नया कुछ ढूँढता है। पर इस बार, कुछ लोग नहीं भूले। थाने की दीवारों पर एक नई नोटिस—“सार्वजनिक शिकायत डेस्क—हर शुक्रवार।” जीप अब भी चलती, पर कुछ धीमी। किसी ठेले पर जाते समय एक नई हिचक। शायद डर। शायद शर्म। शायद दोनों। और वह छोटा-सा ठेला—जिसे अब अनिल ने एक साफ जगह पर लगवा दिया था, एक रिहर्सल स्पॉट की तरह—जहाँ राहुल कभी-कभार अपने पुराने ग्राहक के लिए समोसे बनाता। लोग अब भी कहते—“वही स्वाद!” राहुल हँसता—“अम्मा का मसाला।”
एक बार, किसी पत्रकार ने राहुल से पूछा—“तुम्हारा नाम क्या है—राहुल या अर्जुन?” उसने कुछ पल सोचा। “दोनों,” उसने कहा। “राहुल वह है जिसने समोसे तले, अम्मा को दवा दी, जुल्म का सामना किया। अर्जुन वह है जिसे अपने माता-पिता मिले, जिसने पढ़ाई शुरू की, जिसने वायलिन उठाया। एक मेरा जन्म है, एक मेरा पुनर्जन्म। मैं किसी एक को छोड़कर दूसरे को नहीं चुन सकता।”
रिपोर्टर ने अगला सवाल पूछा—“तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या?”
राहुल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया—“कि न्याय कोई स्वतः होने वाली चीज़ नहीं है। न्याय लोगों से बनता है। पंकज जैसा एक आदमी जब ‘न’ कहता है, तब—” उसने हवा में एक रेखा खींची—“एक दरार बनती है। और उन दरारों से रोशनी आती है।”
वह शाम—जब बंगले के बगीचे में, शारदा अम्मा, अनिल, प्रिया, पंकज का परिवार और कुछ पड़ोसी बैठे थे। राहुल ने ढोलक उठाई। फिर वायलिन। फिर बिना वाद्य के, अपनी पुरानी आवाज़ में एक नया गीत—“समोसा, चटनी, और कानून”—लोग हँसे। उसने गाया—“जो भूख में बाँटता था थप्पड़, अब उसे भूख लगी है शर्म की। जो हक छीन लेते थे हँसकर, अब हक सिखाती है कर्म की।” तालियाँ बजीं—पर अब वे तालियाँ किसी टीआरपी की भूख से नहीं थीं—वे पड़ोस की खालिस दुआओं जैसी थीं।
कुछ दिन बाद, शहर के एक बड़े सभागार में “नागरिक साहस” पर सेमिनार हुआ। मंच पर न्यायाधीश, वरिष्ठ पत्रकार, पुलिस रिफॉर्म पर काम करने वाले एक्टिविस्ट। राहुल वहाँ वक्ता था—कद में छोटा, आवाज़ में बड़ा। उसने बोला—“मैं कानून को दोष नहीं देता। मैं उन लोगों को देता हूँ, जो कानून पहनकर अपनी इंसानियत उतार देते हैं। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ—जो इंसान बने रहते हैं—भले उनका पेशा कुछ भी हो।” पंक्ति खत्म हुई, तालियाँ बजीं। एक पुलिस अधिकारी, जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे, उठे और उनके हाथों से ताली बजी। वे मंच के बाद राहुल से मिले—“बेटा, तुम सही कहते हो। हमें बदलना होगा। हम बदलेंगे।”
राहुल ने वही पुरानी विनम्र मुस्कान दी—“धन्यवाद, साहब। एक बच्चे के लिए, एक ठेले के लिए, एक अम्मा के लिए—कृपया बदल जाइए।”
सेमिनार समाप्त होने के बाद, बाहर लॉबी में पंकज के बेटे रवि ने राहुल को कंधे से ठोका—“कंचे लाया हूँ।” दोनों हँसते हुए नीचे बगीचे में भाग गए। शारदा अम्मा दूर से देखती रहीं—मुस्कान में बीती हुई रातों का धुआँ घुलता गया। अनिल और प्रिया ने एक-दूसरे का हाथ थामा—“घर पूरा है”—उन्होंने मन ही मन कहा।
रात को, जब सब सो गए, राहुल अपने कमरे में बैठा रहा। खिड़की के काँच में शहर की रोशनियाँ छोटे-छोटे तारे जैसी लग रही थीं। उसने डायरी निकाली—पहला पन्ना। उसने लिखा—
“आज मैंने सीखा कि अँधेरा सबसे ज्यादा वहीं होता है जहाँ रोशनी रखने की बात कही जाती है। पर मैं यह भी जानता हूँ कि रोशनी उसी अँधेरे में रखी जाए, तो सबसे ज्यादा जगमगाती है। मैं राहुल हूँ। मैं अर्जुन हूँ। मैं ठेले की गर्मी हूँ। मैं वायलिन की ठंडी तान हूँ। मैं पंकज की हिम्मत हूँ। मैं अम्मा की दुआ हूँ। और मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि कोई और आए। मैं खुद उठूँगा, जो उठ सके, उसे उठाऊँगा।”
उसने पेन रख दिया। कमरे में शांति थी। एक छोटा-सा नाइटलैम्प जल रहा था—पीली रोशनी। बाहर कहीं दूर एक पुलिस सायरन की आवाज़ आई—पर इस बार, वह भय नहीं, सुरक्षा का संकेत लग रही थी। शायद सब नहीं बदलता, पर कुछ तो बदलता है—और कुछ से ही यात्रा शुरू होती है।
सुबह होगी। राहुल फिर उठेगा—स्कूल, अभ्यास, और शायद एक शाम—बंगले के पिछवाड़े में एक छोटा-सा स्टॉल—“अम्मा के समोसे”—फ्री में नहीं, सम्मान से। सामने एक छोटी-सी चिट—“पैसा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, पर हक मत छीने।” लोग आएँगे। चटनी डाली जाएगी। और हँसी इस बार किसी की गरिमा पर नहीं, गरिमा के साथ होगी।
कहानी वहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि न्याय कोई आखिरी पन्ना नहीं, वह तो रोज़ लिखी जाने वाली डायरी है। और राहुल, शारदा अम्मा, पंकज, अनिल, प्रिया—सब उस डायरी के लेखक हैं। कल को कोई और पन्ना किसी और हाथ से लिखा जाएगा। पर शीर्षक वही रहेगा—“लाइनमैन की शपथ”—कि जब भी सिस्टम की तारें जलेंगी, कोई न कोई आकर फ्यूज़ बदल देगा। कोई न कोई, “न” कहेगा। कोई न कोई, वीडियो ऑन करेगा। और फिर—शहर की बत्तियाँ—एक-एक करके, फिर से जल उठेंगी।
News
उस दिन के बाद ऑफिस का पूरा माहौल बदल गया। अब कोई भी किसी की औकात या कपड़ों से तुलना नहीं करता था। सब एक-दूसरे की मदद करने लगे। अर्जुन सबसे प्रेरणा देने वाला इंसान बन गया। रिया भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह विनम्रता से छोटे काम करने लगी और धीरे-धीरे सबका विश्वास जीतने की कोशिश करने लगी।
चायवाले से मालिक तक: इंसानियत की असली पहचान सुबह-सुबह जयपुर शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस के गेट…
रिया फूट-फूट कर रो पड़ी। उसके सारे सपने, घमंड और अभिमान पल भर में टूट गए थे। बाकी सभी कर्मचारी भी कांप गए। सब सोचने लगे, “हे भगवान, हमने भी कल उस चायवाले की हंसी उड़ाई थी। अब अगर मालिक को याद आ गया तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी।”
चायवाले से मालिक तक: इंसानियत की असली पहचान सुबह-सुबह जयपुर शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस के गेट…
दूसरे दिन का माहौल चायवाले से मालिक तक: इंसानियत की असली पहचान
चायवाले से मालिक तक: इंसानियत की असली पहचान सुबह-सुबह जयपुर शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस के गेट…
चायवाले से मालिक तक: इंसानियत की असली पहचान
चायवाले से मालिक तक: इंसानियत की असली पहचान सुबह-सुबह जयपुर शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस के गेट…
I gave a drenched old man shelter in my home. The next morning, he offered to buy my house for $1. “I’m not joking,” he said. “I can’t explain, but you need to leave it immediately.”
I gave a drenched old man shelter in my home. The next morning, he offered to buy my house for…
शीर्षक: “शिखर पर अहंकार नहीं, इंसानियत टिकती है”
शीर्षक: “शिखर पर अहंकार नहीं, इंसानियत टिकती है” सुबह के दस बजे थे। शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट “एमराल्ड टैरेस…
End of content
No more pages to load